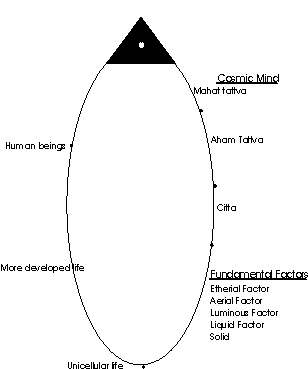पुरुष या चेतना (Consciousness) को इसके द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्यों के अनुसार परिभाषित किया जा सकता है। सर्वप्रथम चेतना ब्रह्मांड की सभी घटनाओं (events) को साक्षी भाव से देखने का कार्य करती है। यह एक कमरे में छत से लटके झूमर में लगे चमकते बल्ब (chandelier bulbs) की तरह है; इसके प्रकाश में कोई जाली चेक पर साइन करता है, कोई ईश्वर की पूजा करता है, लेकिन झूमर के प्रकाश में कोई परिवर्तन नहीं होता। झूमर के चमकते बल्ब का प्रकाश प्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार की क्रिया में भाग नहीं लेता, वह सभी गतिविधियों को संभव बनाता है और सभी गतिविधियों का अवलोकन साक्षी भाव से करता है। यह एक ज्ञानात्मक संकाय (cognitive faculty) है।
चेतना (Consciousness, पुरुष या ब्रह्म) का दूसरा कार्य है कि वह ब्रह्मांड (भौतिक जगत) का उपादान कारण (material cause) भी है; यही वह आधारभूत सामग्री, मूल वस्तु “basic stuff” है जिससे बाकी सब कुछ बना है। वैज्ञानिक लोग हमेशा से ब्रह्मांड के मूलभूत पदार्थ (fundamental matter) की खोज करते आ रहे हैं। एक समय में उन्होंने सोचा था कि परमाणु सबसे छोटा कण है, लेकिन हाल के वर्षों में वे परमाणु को विभाजित और उप-विभाजित कर रहे हैं, और उस छोटे से छोटे कण 'God Particle' की खोज में लगे हुए है, जिसका कोई अंत नहीं है। जबकि हमारे ऋषियों (Yogic scientists) ने हजारों वर्षों पूर्व घोषित किया है कि सभी अस्तित्व का अंतिम कारण और सभी भौतिक वस्तुओं का मूल स्रोत शुद्ध चेतना (pure consciousness) के अलावा और कुछ नहीं है।
चेतना का वर्णन करने का एक और तरीका यह है कि यह उपादान कारण होने के साथ साथ, ब्रह्मांड का "निमित्त कारण" (efficient cause)भी है। यह इस ब्रह्मांड में सभी क्रियाओं को नियंत्रित करने वाली मूलभूत इकाई है। चेतना (Consciousness,पुरुष या ब्रह्म) ही उस मास्टर-वास्तुकार की तरह है जिसने ब्रह्मांड का नक्शा (plan) बनाया है और इसे पूरा करने के लिए कार्य कर रहा है।
हालाँकि, वास्तुकार अपने कार्य को पूरा करने के लिए, क्रियात्मक सिद्धांत प्रकृति (energy, शक्ति या operative principle) की मदद लेता है। सृष्टि के चक्र (cycle of creation) में प्रमुख नियंत्रक भूमिका चेतना (पुरुष) की होती है और सृष्टि क्रमविकास सिद्धांत को चेतना की विशेषता माना जाता है। यह चेतना (Consciousness या ब्रह्म) है जो क्रियात्मक सिद्धांत (प्रकृति) को कार्य करने की अनुमति देता है। यदि चेतना क्रियात्मक तत्त्व को कार्य करने का अवसर नहीं देती है, तो शुद्ध चेतना बिना किसी रूप-परिवर्तन (modification) के पूर्ववत बनी रहती है। लेकिन इस स्थिति में चेतना (परम् सत्य या ब्रह्म) मानवीय अवधारणा से परे (इन्द्रियातीत) है क्योंकि इसमें रूप (आकार या रंग),रस,गंध,शब्द और स्पर्श जैसे गुण नहीं हैं। तंत्र मार्ग में शुद्ध चेतना की इस अवस्था को निर्गुण ब्रह्म कहा जाता है।
जब चेतना (पुरुष या ब्रह्म) क्रियात्मक सिद्धांत (प्रकृति) को कार्य करने की अनुमति देता है, तो वह तीन मौलिक प्रणाली के अनुसार (3 modes according) कार्य करती है। अर्थात प्रकृति मूल शुद्ध चेतना (pure consciousness) को तीन अलग-अलग तरीकों से रूपान्तरित करके इस जगत (नाम-रूप) में विभिन्नता पैदा करती है। क्रियात्मक सिद्धान्त (प्रकृति) के तीन कार्य -प्रणाली को संस्कृत में 'गुण' के नाम से जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है - ' बन्धन में डालने वाले गुण (binding quality)। यह शब्द 'गुण' इस विचार से निकला है कि प्रकृति एक रस्सी (रज्जु) की तरह है जो चेतना (Consciousness) को बंधन में डालकर संशोधित करती है। त्रिगुणों में जब कोई विशेष गुण सक्रिय होता है तो चेतना का परिवर्तन (modification) या बंधन (modification) होता है। प्रकृति के तीन गुणों को सत्व (बोधक्षम, sentient), रजः (mutative-विकारकारी) और तमः (static,गतिहीन) कहा जाता है।
सत्त्वगुण चेतना को बांधने या परिवर्तित करने वाला सबसे सूक्ष्म बंधन है। यह सतोगुण अस्तित्व की भावना-"मैं हूं" “I exist”, के लिए उत्तरदायी है। रजो गुण “I do” - "मैं कर्ता हूँ" की भावना के लिए जिम्मेदार है, और तमो गुण सबकुछ "मैंने किया है" की भावना (अहं) पैदा करता है।तमो गुण विचार को ठोस बनाने का काम करता है और ब्रह्मांड में हम जितने भी ठोस वस्तुओं को देखते हैं, उनके निर्माण के लिए तमोगुण ही जिम्मेदार है।
वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रकृति क्रिया करती है, और चेतना को रूपांतरित करना शुरू करती है सगुण ब्रह्म या गुणों के साथ ब्रह्म (Brahma with qualities) का निर्माण करती है? सबसे पहले, हमें सृष्टि से पहले की अवस्था, ब्रह्मांड निर्माण की "पूर्व" स्थिति की कल्पना करने का प्रयास करना चाहिए। उस अवस्था में सर्वोच्च चेतना (Supreme Consciousness ) बिना किसी रूपांतरण के होती है। प्रकृति के तीनों गुण विद्यमान हैं लेकिन वे क्रियाशील नहीं हैं। यदि तीनों शक्तियों को असंख्य रेखाओं द्वारा दर्शाया जाये, तो इन रेखाओं के परस्पर कटाव (intersections) से गणनातीत बहुभुज क्षेत्र (polygons) बनते हैं। यह उस अवस्था को चित्रित करने का एक सैद्धांतिक तरीका है जिसमें चेतना अपरिवर्तित (unmodified) है।
आगे बढ़ने पर , तीनों शक्तियों द्वारा निर्मित सबसे स्थिर आकृति एक त्रिभुज के रूप में प्राप्त होती है। "शक्तियों के इस त्रिकोण" में तीनों गुण चारों ओर घूम रहे हैं, और स्वयं को एक दूसरे में रूपांतरित करते रहते हैं। पुरुष (Consciousness, चेतना या ब्रह्म ) इस त्रिभुज के अंदर "फंस" गया है। इस त्रिकोण का बनना ब्रह्मांड (जगत) के निर्माण के प्रारम्भ का संकेत देता है।
त्रिभुज के अंदर का पुरुष (चेतना) - पुरुषोत्तम- ब्रह्मांड का केंद्र है। और जब त्रिकोण में शक्तियों का संतुलन भंग हो जाता है, तो एक संवेदनशील शक्ति, त्रिकोण से बाहर निकल जाती है और चेतना को रूपांतरित करती है।
चेतना का यह पहला परिवर्तन बहुत सूक्ष्म है। तब “I exist”- "मैं हूं" की भावना पैदा होती है और चेतना (पुरुष, Consciousness) स्वयं के बारे में जागरूक हो जाता है। इस "मैं हूं" की भावना को महत तत्व कहा जाता है और यह ब्रह्मांडीय मन (माँ जगदम्बा के सर्वव्यापी विराट मैं या अहं) का पहला भाग है। प्रथम परिवर्तन के बाद, दूसरा रजो गुण की शक्ति सक्रिय हो जाती है और चेतना में एक और गुण जुड़ जाता है। शुद्ध चेतना में यह विचार उत्पन्न होता है कि "मैं कर्ता हूँ" फिर ब्रह्मांडीय मन ( Cosmic Mind) का दूसरा भाग - अहं तत्व - निर्मित होता है।अंत में, तीसरा गुण - स्थैतिक शक्ति या तमो गुण - सक्रिय हो जाता है और चेतना को दूसरे तरीके से परिवर्तित करता है। और चेतना में यह "मैंने किया है" -“I have done” की भावना उत्पन्न करता है। यह ब्रह्मांडीय मन के तीसरे भाग- चित्त या मन वस्तु ( mind stuff) का निर्माण करके चेतना (पुरुष) को विषयाश्रित करता है।
ब्रह्मांडीय मन (Cosmic Mind) का यह वर्णन अमूर्त विचार लग सकता है, लेकिन अगर हम अपने स्वयं के मन की कार्यप्रणाली को समझ सकें, जो कि ब्रह्मांडीय मन का एक छोटा संस्करण है, तो हम इसे बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। दर्शन क्रिया कैसे होती है ? यदि हम किसी बरगद के विशाल वृक्ष को देखते हैं , तो यह दर्शन क्रिया वास्तव में कैसे हो रही है ? हमारे आँखों की पुतलियों को वृक्ष से परावर्तित प्रकाश प्राप्त हो रहा है और यह मस्तिष्क में अवस्थित दर्शन इन्द्रिय तक पहुँचाया जाता है और अंत में हमारा मन भी उससे जुड़ा हुआ हो तभी उस मन में वृक्ष की एक स्पष्ट छवि बनती है। हालाँकि, हम अपनी आँखें मूँदकर भी अपने मन में वृक्ष की छवि ला सकते हैं। मन का वह भाग जो मन में वृक्ष को "बनाने" का आदेश देता है, वह "मैं कर्ता हूँ", “I do” factor, कारक या अहं तत्व है, जिस पर परिवर्तनशील रजोगुण का बर्चस्व है। उसी प्रकार पूर्व में सूंघे गए गुलाब के फूल के सुगन्ध को भी अपने मन में ला सकते हैं। मन का वह भाग जो वृक्ष की छवि बनाता है, या गुलाब के सुगन्ध का स्मरण करता है,वह चित्त या "मैंने किया है" का साधन (factor) है। चित्त एक पर्दे (screen) की तरह है जिस पर "मैं करता हूं" “I do” factor. कारक के आदेशों के अनुसार छवियां बनती हैं। और मन की सभी क्रियाओं में, "मैं हूँ" “I exist” या महत् तत्व मौजूद होना चाहिए, क्योंकि "मैं" हूँ के भाव के बिना कोई भी "मैं कर्ता हूँ" “I do”नहीं हो सकता।
इस प्रकार, ब्रह्माण्डीय मन ( Cosmic Mind) भी हमारे व्यक्तिगत मन (individual mind) की तरह ही कार्य करता है, लेकिन एक महत्वपूर्ण अंतर है जिस पर यहां ध्यान दिया जाना चाहिए। जैसा कि हमने ऊपर चर्चा की, भौतिक जगत (जैसे विशाल बरगद का पेड़) हमें अपने व्यक्तिगत चित्त रूपी पर्दे पर अंकित बाह्य सत्य के रूप में दिखाई देता है, उसी प्रकार ब्रह्मांडीय मन (Cosmic Mind) के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड विशाल ब्रह्मांडीय चित्त (cosmic citta) पर अंकित एक आंतरिक छवि (internal image) है। इसके अलावा, हमारे व्यक्तिगत मन में अगर हम हरे हाथी (green elephant) को बनाने के लिए अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करते हैं, तो यह छवि किसी दूसरे मन के लिए वास्तविकता नहीं है, सिवाय उस मन के जिसने इसकी कल्पना की थी। लेकिन अगर ब्रह्मांडीय मन के ब्रह्माण्डीय चित्त (cosmic citta) में हाथी की कोई छवि है, तो यह एक वास्तविकता है और सूक्ष्म-ब्रह्मांडीय इकाई मनों (micro-cosmic unit minds) के द्वारा भी ऐसा ही माना जाएगा।
ब्रह्मांडीय मन के तीन भागों के गठन के बाद, स्थैतिक शक्ति ( static force) या तमो गुण ब्रह्मांडीय मन के चित्त भाग को परिवर्तित करना जारी रखता है और शुद्ध चेतना में और भी गुणों को जोड़ता है। यह चित्त के एक हिस्से को पांच मौलिक कारकों (five fundamental factors) में रूपांतरित करना शुरू कर देता है। तांत्रिक मार्ग में पाँच मूलभूत कारक कहे गए हैं।
पहले को ईथर (etherial factor) या आकाश तत्व के रूप में जाना जाता है। हालांकि आधुनिक विज्ञान ने 19वीं शताब्दी के मिशेलसन-मॉर्ले प्रयोगों (Michelson-Morley experiments) के बाद इसका पता लगाने में विफल होने के बाद ईथर की अवधारणा को त्याग दिया। हम आधुनिक विज्ञान के साथ योग प्रणाली के आकाश तत्व को "अंतरिक्ष"-“space” या खाली जगह के रूप में सोच कर सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। तंत्र मार्ग में इस स्थानिक कारक (spatial factor) को ओंकार या ॐ शब्द के रूप में जाना जाने वाला सूक्ष्म आद्य स्पंदन (primordial vibration) ले जाने में सक्षम कहा जाता है।
चूंकि तमोगुण चेतना को परिवर्तित करना जारी रखता है, चेतना (Consciousness) का एक हिस्सा वायु तत्व या गैसीय कारक में परिवर्तित हो जाता है। यह वायु तत्व शब्द और स्पर्श (sound and touch) के कंपन का वाहक होता है। अगला कारक तेजस तत्त्व या अग्नि कारक है। यह तेजस कारक (luminous factor) शब्द, स्पर्श और दृष्टि (रूप) कंपन का वाहक होता है। तेजस कारक के बाद तरल कारक (liquid factor) 'आपो ' या जल तत्त्व' का निर्माण करता है, जो स्वाद (रस) कंपन के साथ-साथ शब्द, स्पर्श और रूप के स्पंदन को भी वहन करता है। अंतिम कारक, ठोस या 'क्षिति तत्त्व' पृथ्वी जो गंध कंपन के साथ-साथ अन्य कारकों द्वारा किए गए कंपन का भी वहन करता है।
इस प्रकार, इस भौतिक जगत की सभी वस्तुएं ब्रह्मांडीय मन के चित्त में मौजूद हैं। और इस भौतिक जगत को ब्रह्मांडीय चेतना ( Cosmic Consciousness) का एक विचार प्रक्षेपण (thought projection) माना जा सकता है। आधुनिक विज्ञान भी इसी स्थिति को स्वीकार करने की ओर बढ़ रहा है। भौतिक विज्ञानी सर जेम्स जीन्स [ Physicist Sir James Hopwood Jeans (11 September 1877 – 16 September 1946) ], ने अपनी पुस्तक "The Mysterious Universe' में लिखा है- द ऑब्जर्वर (लंदन) में प्रकाशित एक साक्षात्कार में, जब उनसे यह सवाल पूछा गया कि "क्या आप यह मानते हैं कि इस ग्रह पर जीवन किसी प्रकार की 'दुर्घटना का परिणाम' है, या क्या आप यह मानते हैं कि ब्रह्माण्ड (जगत) किसी 'उत्कृष्ट योजना' का हिस्सा है?"... उन्होंने उत्तर दिया: मैं आदर्शवादी सिद्धांत की ओर झुकता हूं कि " चेतना मौलिक है, और भौतिक ब्रह्मांड चेतना से व्युत्पन्न है, न कि भौतिक ब्रह्मांड से चेतना ... क्योंकि “ज्ञान की धारा एक अयांत्रिक वास्तविकता (non-mechanical reality) की ओर बढ़ रही है; और ब्रह्मांड एक 'विशाल मशीन' (great machine) की तुलना में एक 'उत्कृष्ट विचार' (great thought) की तरह अधिक दिखने लगा है। "(The stream of knowledge is heading towards a non-mechanical reality; the universe begins to look more like a great thought than like a great machine. https://dsguruji.com/tidal-hypothesis-of-jeans-and-jeffreys/)
जब चेतना एक ठोस कारक (पृथ्वी-क्षिति) में परिवर्तित हो जाती है तो ब्रह्मांडीय चक्र (cosmic cycle ) का आधा हिस्सा पूरा हो चुका होता है। ब्रह्मांडीय चक्र (cosmic cycle) के पहले भाग में चेतना ब्रह्मांडीय मन (Cosmic Mind) में परिवर्तित हो जाती है, और फिर पंच महाभूतों में। इस प्रक्रिया सिनकारा (saincara) या "ब्रह्मांडीय नाभिक (cosmic nucleus) से दूर होने वाली गतिविधि " के रूप में जाना जाता है। ब्रह्माण्डीय चक्र के दूसरे भाग में, पदार्थ पुनः शुद्ध चेतना (pure Consciousness) में परिवर्तित हो जाता है। ब्रह्माण्ड के केंद्रक ( nucleus of the universe) की ओर इस गति को प्रतिसिंकरा (pratisaincara) के रूप में जाना जाता है।
पहले हमने देखा था कि तीन गुणों या बंधन कारी सिद्धांतों ( binding principles) की प्रक्रिया के माध्यम से चेतना (Consciousness) ब्रह्मांडीय मन (Cosmic Mind) में परिवर्तित हो जाती है और ब्रह्मांडीय मन का एक हिस्सा ब्रह्मांड का निर्माण करने वाले मूल तत्वों (पंच महाभूतों) में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन चेतना (Consciousness) के निर्जीव (inanimate-अचेतन) वस्तुओं में परिवर्तन के साथ ही सृजन की प्रक्रिया समाप्त (The process of creation does not stop) नहीं हो जाती। प्रकृति के तीनों गुण या बाध्यकारी सिद्धांत (The binding principles) चेतना को रूपांतरित करने की प्रक्रिया जारी रखते हैं , और इसी प्रक्रिया द्वारा सजीव प्राणियों का क्रम -विकास होता रहता है।
यह प्रकृति के तमो गुण का स्थिर सिद्धांत (static principle)ही है, जो चेतना के निरंतर परिवर्तन को जारी रखता है। संस्कार चरण (saincara phase) के अंत में हम ठोस कारक (पृथ्वी) का निर्माण पाते हैं। तमो गुण ठोस वस्तुओं पर दबाव डालता है, उन्हें संकुचित करने या अणुओं के बीच की जगह ( space between the molecules) को कम करने का प्रयास करता है। स्थैतिक सिद्धांत का यह संपीड़न (compression या दबाव ) वस्तुओं के भीतर शक्तियों (आकर्षण और विकर्षण शक्ति) के निर्माण का कारण बनता है। वस्तु पर दबाव के एक शक्ति को "बाह्य" शक्ति (exterial -केन्द्राप्रसारी) कहा जाता है, एक प्रकार की सैन्यशक्ति वस्तु के केंद्र से बाहर की ओर गति करता है और वस्तु को तोड़ने का कार्य करता है। एक अन्य शक्ति को "आंतरिक" (केन्द्राभिसारी-interial) कहा जा सकता है - क्योंकि यह वस्तु को एक साथ रखने के लिए कार्य कर रहा है और यह वस्तु के नाभिक (object’s nucleus) की ओर दबाव बढ़ाता है। इन दोनों शक्तियों का (केन्द्राभिसारी और केन्द्राप्रसारी शक्तियों का) सम्मिलित नाम (collective name ) 'प्राण' है।
यदि केन्द्राभिमुख आंतरिक शक्ति (center-seeking interial force) प्रबल हो तो ठोस कारक में एक केन्द्रक (nucleus) बनता है और यही केन्द्रक वस्तु के भीतर प्राण या जीवनी-शक्ति ( vital force) को नियंत्रित करता है, और अब उस पदार्थ में जीवन के क्रम-विकास की सम्भावना उतपन्न होती है। हालांकि, केन्द्रा-प्रसारी शक्ति (exterial-seeking force) यदि अधिक शक्तिशाली (stronger) है, तो परिणामी शक्ति (resultant force) वस्तु में विस्फोट उत्पन्न कर देता है।
संस्कृत में वस्तु को तोड़ देने वाले अपरिष्कृत कारक (crude factor) को जड़-स्फोट के रूप में जाना जाता है - और विस्फोट से मरने वाले सितारों को खगोलविद की भाषा में सुपरनोवा कहा जाता है। खगोलविदों के अनुसार जब कोई प्राचीन सितारा अपना जीवन-चक्र समाप्त करके अपने जीवनकाल के अंतिम चरण में होता है, तो वह एक भयंकर विस्फोट के साथ समाप्त हो जाता है जिसे सुपरनोवा कहते हैं। जो जड़-स्फोट के उदाहरण हैं। (supernova-एक ऐसा तारा जिसकी चमक अचानक बहुत बढ़ जाती है क्योंकि एक विनाशकारी विस्फोट होता है जो अपने अधिकांश द्रव्यमान को बाहर निकाल देता है। जड़-स्फोट के कारण ठोस कारक (solid-factor,क्षिति) तरल (liquid), आकाशज (aerial या etherial), और प्रकाशमान (luminous) कारकों में टूट जाता है।)
जीवन के निर्माण के साथ हम ब्रह्मांडीय चक्र ( cosmic cycle) में एक महत्वपूर्ण घटना पाते हैं। प्रत्येक जीव (living entity) में एक 'मन' होता है। जितनी सरल भौतिक संरचना में वह जीवसत्ता होगी, उतना ही सरल उसका मन होगा। इसके विपरीत, किसी इकाई की भौतिक संरचना जितनी जटिल होगी, उसका मन भी उतना ही जटिल होगा।
>>> origin of the mind: प्रत्येक जीवित प्राणी में मन की उत्पत्ति कैसे होती है? वस्तु के भीतर इन केन्द्राभिसारी और केन्द्राप्रसारी के संघर्ष के कारण उत्पन्न घर्षण के परिणामस्वरूप, ठोस का कुछ हिस्सा कुछ सूक्ष्म में चूर्णित हो जाता है (pulverized, पिस जाता है), जिसे 'मन वस्तु' (mind stuff) या चित्त कहते हैं। जैसा कि हम जानते है सभी ठोस पदार्थ (the Cosmic Mind) ब्रह्मांडीय मन से उत्पन्न हुए हैं, यह कहना बिल्कुल सुसंगत और तार्किक है कि इकाई या व्यक्तिगत मन पदार्थ से बाहर आया है, क्योंकि पदार्थ की उत्पत्ति मन से हुई है और इस प्रकार मानसिक क्षमता ( mental potentiality) सभी पदार्थों ( matter) में निहित (inherent) है।
एक कोशिकीय जीवों में ( one-celled living beings में ) जो मन विद्यमान है, वह बहुत सरल है। उदाहरण के लिए, एक प्रोटोजोआ में, हम देख सकते हैं कि इसका व्यवहार सहज या जन्मजात (instinctive) होता है। यदि आप उसके पास गर्म सुई रखते हैं, तो वह अपने आप दूर चली जाती है। इस प्रकार के प्रतिवर्त व्यवहार (reflexive behavior) को उसके सरल मन द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो पूरी तरह से चित्त से बना होता है। "मैं हूं" “I exist” और "मैं कर्ता हूं" “I do” की भावना एककोशिकीय प्राणियों (unicellular beings) में अभिव्यक्ति नहीं पाती है।
जीवन क्रम-विकास (evolution) की स्थिति में है। संघर्ष (conflict) और संसक्ति (cohesion-लगाव) के कारण सरल जन्तु और पौधे अधिक जटिल हो जाते हैं। तंत्र मत में हम यह भी अवलोकन करते हैं कि तमो गुण, जो ब्रह्मांडीय चित्त (cosmic citta) के बिंदु से सरल जीवन के निर्माण के बिंदु तक सृष्टि के चक्र पर हावी रहता है, वह इस चरण में अपना प्रभुत्व खो देता है। रजो गुण, या परिवर्तनकारी शक्ति, अब प्रभावी हो जाती है। इस अवस्था में जीव शारीरिक रूप से अधिक से अधिक विकसित हो जाते हैं, और साथ ही उनका मन भी अधिक जटिल हो जाता है। पशुओं और पौधों में न केवल एक मन होता है जो सहज और प्रतिवर्त व्यवहार को नियंत्रित करता है बल्कि अब मन के दूसरे कार्यात्मक भाग "मैं कर्ता हूँ" (अहं तत्त्व) का भी अस्तित्व है। जब "मैं कर्ता हूं" कारक को (मनोविज्ञान में "अहंकार" के रूप में भी जाना जाता है) जो मन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। और यह मात्रा में मन-वस्तु चित्त की तुलना में अधिक होता है जो वृत्ति को नियंत्रित करता है, इसलिए पशुओं में भी बुद्धिमानी पूर्ण व्यवहार करने की क्षमता होती है। जैसे-जैसे अहम् तत्त्व अधिक विकसित होता जाता है, वैसे-वैसे पशुओं (बुलडॉग कुत्तों का ?) का व्यवहार और अधिक जटिल होता जाता है।
क्रम-विकास (Evolution) जारी रहता है, और हम देखते हैं कि कुछ जानवरों और पौधों में मन के दूसरे हिस्से की अभिव्यक्ति भी होती है। मन का यह अधिक क्रमविकास सबसे सूक्ष्म और सबसे शक्तिशाली गुण, सत्व गुण की बढ़ती हुई गतिविधि के कारण होता है। सत्त्व गुण के प्रभाव से “I exist” "मैं हूँ" कारक (महत तत्व) का निर्माण होता है। यदि किसी प्राणी के मन में महत तत्व की मात्रा अहम् तत्त्व की मात्रा से अधिक होती है, तो उसका अतिरिक्त भाग (surplus portion) जीव में सहज ज्ञान युक्त संकाय ( intuitive faculty ) के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। जबकि बुद्धि एक विश्लेषणात्मक संकाय ( analytical faculty) है, और अंतःस्फुरण (अन्तर्ज्ञान) एक संयोगात्मक संकाय (synthetic faculty) है। बुद्धि से हम किसी वस्तु को उसके अंशों की जांच करके जान सकते हैं जबकि अंतर्ज्ञान से किसी चीज को उसकी समग्रता में, अखण्ड रूप (holistic manner) से जानना संभव है। मनुष्यों में जिनके पास बहुत अधिक अंतर्ज्ञान है, उन्हें हम संत (ऋषि ) के रूप में पहचानते हैं।
विकसित अंतर्ज्ञान (developed intuition) वाले सन्तों या ऋषियों में पाई जाने वाली दो महत्वपूर्ण विशेषताएं है विवेक और वैराग्य। (सन्त की पहचान discrimination,शाश्वत-नश्वर विवेक, श्रेय-प्रेय विवेक और वैराग्य यानि अहं का त्याग (renunciation) या तीनों ऐषणाओं से अनासक्ति ( non-attachment) हैं।
>> श्वेताश्वतर उपनिषद् में 'ब्रह्म-चक्र' के माध्यम से त्रैतवाद की व्याख्या : *साभार : @ उत्तरा नेरुरकर /Uttara Nerurkar/
( https://www.indianvedas.net/article/upanishads/)
सौ से अधिक उपनिषदों में से दस मुख्य माने गए हैं, इसलिए कि शंकराचार्य ने उनके भाष्य लिखे हैं । अवश्य ही वे उस समय प्रसिद्धतम होंगे, इसीलिए उन्होंने उनपर भाष्य भी लिखे । लेकिन एक उपनिषद् और भी है जिसपर शंकर ने भाष्य लिखा । वह है श्वेताश्वतर । मानव मन का पुरातन प्रश्न है – "हम कहां से आए हैं और कहां जा रहे हैं ?" – इसी प्रश्न को इस उपनिषद में भी उठाया गया है, और उसका उत्तर भी बहुत स्पष्ट तरीके से दिया गया है ।
ॐ ब्रह्मवादिनो वदन्ति॥
किं कारणं ब्रह्म कुतः स्म जाता जीवाम केन क्व च संप्रतिष्ठाः।
अधिष्ठिताः केन सुखेतरेषु वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम्॥
(श्वेताश्वतरोपनिषद् 1.1)
अन्वय -ब्रह्मवादिनः वदन्ति किम् कारणम् ब्रह्म कुतः जाताः स्मः केन जीवामः क्व च सम्प्रतिष्ठा केन अधिष्ठिताः सुखेतरेषु ब्रह्मविदः व्यवस्थां वर्तामहे॥
Rishis, discoursing on Brahman, ask: Is Brahman the cause? Whence are we born? By what do we live? Where is our final rest? O ye who know Brahman, under whose guidance we abide by the law of happiness and misery.
-ब्रह्म पर चर्चा करते हुए ऋषिगण प्रश्न करते हैं: क्या ब्रह्म (जगत का) कारण है? हम कहाँ से उत्पन्न हुए, किसके द्वारा जीवित रहते हैं और अन्त में किसमें विलीन हो जाते हैं? हे ब्रह्मविदो! वह कौन अधिष्ठाता है जिसके मार्गदर्शन में हम सुख-दुःख के विधान (law of happiness and misery) का पालन करते हैं?
यह उपनिषद् सम्भवतः सब उपनिषदों में से सबसे स्पष्ट रूप से परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति (माँ जगदम्बा) का व्याख्यान करता है । ध्यान की प्रक्रिया भी यहां स्पष्ट शब्दों में दी गई है । काव्यात्मक दृष्टि से भी यह अति सुन्दर है । इसके श्लोक अनेकों प्रकरणों में दौहराए जाते हैं । अनन्य भक्ति से ये सभी ओत-प्रोत हैं । इस उपनिषद् में अधिकतम वेद-मन्त्र भी उल्लिखित हैं । चुने हुए सबसे बढ़िया वेद-मन्त्र यहां होने के कारण, जो भी वेदों से परिचित होना चाहता है, उसे इस उपनिषद् को अवश्य पढ़ना चाहिए ।
त्रैतवाद का प्रधान उपमात्मक वेदमन्त्र यहां जैसा का तैसा दिया गया है –
द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया
समानं वृक्षं परिषस्वजाते ।
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्ववत्त्य-
नश्नन्नन्यो अभिचाकशीति ॥ ४।६ ॥
अन्वय -द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते। तयोः अन्यः पिप्पलं स्वादु अत्ति। अन्यः अनश्नन् अभिचाकशीति॥
अर्थात् दो सुन्दर पंखों वाले पक्षी, जो साथ-साथ रहने वाले तथा परस्पर सखा हैं, समान वृक्ष पर ही आकर रहते हैं; उनमें से एक उस वृक्ष के स्वादिष्ट फलों को खाता है, दूसरा खाता नहीं है, केवल देखता है।
(इस व्यक्त जगत में) दो सुन्दर गुण-रूपी पंखों वाले पक्षी हैं (परमात्मा और जीवात्मा), जो कि साथ-साथ रहते हैं और एक-दूसरे के सखा हैं, एक ही वृक्ष (जगत) से घनिष्ठ सम्बन्ध रखते हैं । उनमें से एक (जीव) तो पेड़ के फलों (सांसारिक भोगों) को स्वाद ले-लेकर खाता है, जबकि दूसरा, बिना कुछ भी खाए हुए, उसको देखता रहता है । बड़े संक्षेप में और बहुत ही सुन्दरता से इस मन्त्र में तीन अस्तित्वों और उनके सम्बन्ध का वर्णन हो जाता है !
श्वेताश्वतर ऋषि ने इसको और भी आगे बढ़ाया, और कहा –
समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो-
ऽनीशया शोचति मुह्यमानः ।
जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीश-
मस्य महिमानमिति वीतशोकः ॥ ४।७ ॥
उसी वृक्ष पर पुरुष, अर्थात् जीवात्मा, तो भोगों में निमग्न रहता है । इस कारण वह प्रकृति के वशीभूत होकर, सांसारिक वस्तुओं से मोह करता हुआ, दुःखों को प्राप्त होता रहता है । परन्तु जब वह, अपने द्वारा ध्यान से सेवित किए जाने पर, अपने से अन्य ईश को देखता है, और उसकी महिमा का उसको बोध होता है, तब वह सब शोकों से दूर हो जाता है । कितनी सुन्दरता से ऋषि ने, वेद-मन्त्र की शैली में ही, परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग बता दिया ! साथ-साथ उन्होंने परमात्मा और जीवात्मा की भिन्नता को विस्पष्ट कर दिया । इनको अब एक बताना मूर्ख ही करेगा !
इससे पूर्व श्वेताशतर ऋषि ने एक और श्लोक रचा है –
अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां
बह्वीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः ।
अजो ह्येको जुषमाणोऽनुशेते
जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः ॥ ४।५ ॥
अन्वय - अजाम् एकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्विः प्रजाः सृजमानाम् सरूपाः। अजः एकः जुषमाणः अनुशेते। जहाति एनां अन्यः भुक्तभोगां अजः ॥
ऐसी 'एक' अजा अजन्मी बकरी (प्रकृति) है जो श्वेत-कृष्ण एवं लोहितवर्णा है, जो निरन्तर अनेकरूपा प्रजाओं की सृष्टि करती जा रही है और उसका एक अज बकरा (पुरुष) उसके साथ प्रेम में साहचर्य सुखभोग करता है; जब कि दूसरा अजात (पुरुष) उसके समस्त सुखों का भोग करके उसे त्याग देता है।
(इस ब्रह्माण्ड में) एक अजन्मी, या उपमा से, एक अजा = बकरी (प्रकृति) है जो कि लाल, सफेद और काले रंग (अर्थात त्रिगुण - रज, सत्त्व और तम) वाली है । वह अपने जैसे रूप में बहुत प्रजाओं (वस्तुओं) को सृजती है, जन्म देती है ।
एक अजन्मा, या अज = बकरा (जीवात्मा), उसका भोग करता हुआ लेटता है, जबकि दूसरे एक अजन्मे बकरे (जीवात्मा), ने पहले ही उस बकरी का भोग करके उसको त्याग दिया है । जहां यह उपमा जीव और प्रकृति के सम्बन्ध में विस्पष्ट है ही, वहां यह देखने योग्य है कि विरक्त आत्मा का ब्रह्म से एकत्व नहीं कहा गया है – उसे अलग ही माना गया है ।
’अजन्मा’ होने का भी अर्थ है कि आत्मा किन्हीं वस्तुओं के संयोग या परिणाम से नहीं उत्पन्न नहीं हुआ है, परन्तु उसकी सत्ता भी अनादि है । यदि जीवात्मा परमात्मा का विकार होता तो उसे जन्म-वाला ही मानना पड़ता, जिस प्रकार प्रकृति के सभी विकारों का ’जन्म’ बताया गया है । इसी प्रकार प्रकृति को भी ’अजा’ कहा गया है । उसको परमात्मा मानना तो घोर मूर्खता है !
अन्य एक श्लोक तीनों सत्ताओं में भेद बताता है –
ज्ञाज्ञौ द्वावजावीशनीशा –
वजा ह्येका भोक्तृभोग्यार्थयुक्ता ।
अनन्तश्वात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता
त्रयं यदा विन्दते ब्रह्मेतत् ॥ १।९ ॥
अर्थात् दो अज हैं, एक तो ज्ञ है – जानने वाला है, सर्वज्ञ है; दूसरा अज्ञ है – कम जानता है ; एक सब पदार्थों का प्रभु है, दूसरा उसके वश में रहता है ; और तीसरी एक अजा भोक्ता के भोग के लिए युक्त होती है । जब यह जीव, जो कि अनन्त आत्मा है, अनेक शरीर धारण करने से ’विश्वरूप’ है और अकर्ता है (क्योंकि शरीर ही कर्ता है), इन तीनों सत्ताओं को जान लेता है, तब वह ब्रह्म को पा लेता है । इससे स्पष्ट रूप से और क्या कहा जा सकता है ?!
अन्य एक सुप्रसिद्ध श्लोक परमात्मा का स्वरूप बताता है –
न तस्य कार्यं करणं च विद्यते
न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते ।
परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते
स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ॥ ६।८ ॥
अर्थात् उस परमात्मा का न कार्य, न करण है । उसके बराबर ही कोई नहीं दिखता, तो उससे अधिक का तो कहना ही क्या ! उसकी शक्ति सबसे अधिक है और विविध प्रकार की है, ऐसा वेदादि शब्द प्रमाण हैं । उसमें ज्ञान, बल और क्रिया स्वाभाविक रूप से वर्तमान है । जैसे जीव में प्रकृति के सहारे से ज्ञान, बल और क्रिया होती है, ऐसा परमात्मा के विषय में सत्य नहीं है । इस पूरे ही वर्णन से स्पष्ट है कि जीवात्मा कभी भी परमात्मा का विकार नहीं हो सकता । जिसका कार्य ही नहीं है, तो विकार कैसे मानें ?! जिसका कोई सहाय के लिए उपकरण नहीं है, जिसके कोई बराबर नहीं है, जिसकी शक्ति अपार है, जिसका ज्ञान, बल और क्रिया अपने स्वरूप से ही है, वह एक क्षुद्र प्राणी में कैसे संकुचित हो जायेगा ?
तथापि एक श्लोक है जिसमें यह सन्देह होता है कि सम्भवतः अद्वैतवाद का ऋषि समर्थन कर रहे है –
एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्मसंस्थं
नातः परं वेदितव्यं हि किञ्चित् ।
भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा
सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत् ॥ १।१२ ॥
जिसका अर्थ है – यह देव (पिछले श्लोक से), जो सदा ही हमारी आत्मा के अन्दर बैठा होता है, जानने योग्य है । इससे बढ़कर कुछ भी जानने योग्य नहीं है । भोक्ता (जीवात्मा), भोग्य (प्रकृति) और प्रेरिता (परमात्मा) को जानकर, सब (जान लिया जाता है) । (इस प्रकार) यह तीन प्रकार का ब्रह्म कहा गया है । सो, यहां यह समझा जा सकता है कि ये तीनों ब्रह्म के ही रूप हैं । यहां ’ब्रह्म’ से ’परमात्मा’ समझना इसलिए गलत है क्योंकि, इससे पहले, श्लोक के बाद श्लोक में भोक्ता, भोग्य और प्रेरिता के भेद को पुनः पुनः कहा गया है । १।६ में भी स्पष्टतः कहा गया है –
सर्वाजीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते अस्मिन्हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे।
पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति॥
(श्वेताश्वतरोपनिषद् 1.6)
अन्वय - सर्वाजीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते अस्मिन् ब्रह्मचक्रे हंसः भ्राम्यते। पृथगात्मानम् च प्रेरितारं मत्वा ततः तेन जुष्टः अमृतत्वम् एति॥
इस श्लोक में ब्रह्माण्ड को ’ब्रह्मचक्र’ कहा गया है, जिसको कि परमात्मा घुमाता है । अतएव इस श्लोक में ’ब्रह्म’ का अर्थ ’परमात्मा’ न होकर, ’ब्रह्माण्ड’ ही है ।
उस ब्रह्म चक्र में जो सबका जीवन और आश्रय है हंस (यात्री जीवात्मा) भ्रमण कर रहा है। जब वह अपनी वैयष्टिक आत्मा (जीवात्मा) को पृथक् कर अपने स्वयं को प्रेरक शक्ति (परमात्मा) के रूप में अनुभव करने लगता है तब वह उसकी कृपा से अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है।
In this infinite wheel of Brahman, in which everything lives and rests, the pilgrim soul is whirled about. Knowing the individual soul, hitherto regarded as separate, to be itself the Moving Force, and blessed by Him, it attains immortality. जो अपने को ब्रह्म से भिन्न मानता है वह अज्ञानी है। He who considers himself to be different from Brahman is ignorant.
नीचे दिए वैदिक मन्त्र, जिनका उल्लेख उपनिषद् में हुआ है, को भी अद्वैतवाद में लागु किया जा सकता है –
त्वं स्त्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी ।
त्वं जीर्णो दण्डेन वञ्चसि त्वं जातो भवसि विश्वतोमुखः ॥ ४।३ ॥
'तुम' ही स्त्री हो तथा 'तुम' ही पुरुष हो; 'तुम' ही कुमार हो एवं 'तुम' ही पुनः कुमारी कन्या हो; 'तुम' ही तो जरा-जीर्ण वृद्ध पुरुष हो जो अपने दण्ड के सहारे झुककर चलता है। अहो, 'तुम' ही तो जन्म लेते हो तथा सम्पूर्ण विश्व तुम्हारे ही नाना रूपों से परिपूर्ण है।
वस्तुतः सर्वत्र, श्वेताश्वतर ऋषि ने परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति की भिन्न सत्ता, उनके भिन्न गुण-कर्म-स्वभाव को दर्शाया है । उन्होंने यह भी कहा है कि परमात्मा की शक्ति अपने ही गुणों से छुपी हुई है-
ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्ह्देवात्मशक्तिं स्वगुणैर्निगूढाम्।
यः कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्येकः॥
(श्वेताश्वतरोपनिषद्/१.३)
अन्वय - ते ध्यानयोगानुगताः अपश्यन् स्वगुणैः निगूढां देवात्मशक्तिम्, कालात्मयुक्तानि निखिलानि तानि यः एकः कारणानि अधितिष्ठति॥
तब ऋषियों ने एकाग्रचित्त होकर ध्यान योग में स्वयं भगवान की सृजन-शक्ति को देखा जो अपने गुणों में छिपी हुई थी। ये वही एकमेवाद्वितीयं हैं जो काल, आत्मा तथा सभी कारणों के अधिपति हैं। – देवात्मशक्तिं स्वगुणैर्निगूढाम् (१।३), और यह कि उसे ध्यान-समाधि में ही पाया जा सकता है । इस पर भी विशेष ध्यान देना आवश्यक है – यदि इस संसार में परमात्मा को बुद्धि से, या मन से, ढूढ़ेंगे, तो हमें कभी भी कुछ भी हाथ नहीं लगेगा ! इसलिए इस उपनिषद् में ध्यान लगाने की प्रक्रिया - "मनःसंयोग" का भी विषद वर्णन है ।
दुर्गा पंचरत्नम स्तोत्रम्
(Durga Pancharatnam Stotram) -
ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन् ,त्वामेव देवीं स्वगुणैर्निगूढाम् ।
त्वमेव शक्तिः परमेश्वरस्य,मां पाहि सर्वेश्वरि मोक्षदात्रि ॥ १॥
ध्यान (ध्यान) और चिंतन (योग) अपनाने वाले, या मनःसंयोग का नियमित अभ्यास करने वाले योगियों ने देखा, आप ही एकमात्र माँ जगदम्बा हैं जो अपने ही गुणों में छुपी हुई हैं। और हे जगन्माता दुर्गा (माँ सारदा) आप सभी की माँ हैं, आप ब्रह्मांड के महान भगवान (अवतार वरिष्ठ श्रीरामकृष्ण) के पीछे स्थित एकमात्र शक्ति हैं, इसलिए मोक्ष दातृ माँ सारदा कृपया मेरी रक्षा करें।
देवात्मशक्तिः श्रुतिवाक्यगीता,महर्षिलोकस्य पुरः प्रसन्ना ।
गुहा परं व्योम सतः प्रतिष्ठा,मां पाहि सर्वेश्वरि मोक्षदात्रि ॥ २॥
आप ठाकुर देव की आत्म शक्ति हैं, जिसके बारे में वेदों ने गाया है, बड़े-बड़े संतों (स्वामी विवेकानन्द आदि गुरु ) के सामने तुम्हें प्रसन्न करने से वे प्रसन्न होते हैं, जिन्होंने स्वयं को सत्य के रूप में अपने हृदय में स्थापित किया है,और इसलिए हे सभी की माता, और मुक्ति-भक्ति प्रदायनी माँ श्रीसारदा कृपया मेरी रक्षा करें ।
परास्य शक्तिः विविधैव श्रूयसे,श्वेताश्ववाक्योदितदेवि दुर्गे ।
स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया ते,मां पाहि सर्वेश्वरि मोक्षदात्रि ॥ ३॥
हे माँ सारदा , आप भगवान श्री रामकृष्णदेव की परा नामक शक्ति हैं, जिन्हें --नवनीदा 'सीता, राधा, सरस्वती' आदि विभिन्न नामों से पूजा करते थे, जिनकी स्तुति करते थे । श्वेताशतर उपनिषद में पूजित जाग्रत देवी दुर्गा आप ही हैं। आप अपने स्वभाव से ही , समस्त क्रिया और ज्ञान के पीछे की शक्ति हैं ,और इसलिए हे सभी की 'अपनी माँ', और मुक्ति के दात्री , कृपया मेरी भी रक्षा करें।
देवात्मशब्देन शिवात्मभूता, यत्कूर्मवायव्यवचोविवृत्या ।
त्वं पाशविच्छेदकरी प्रसिद्धा,मां पाहि सर्वेश्वरि मोक्षदात्रि ॥ ४॥
भगवान श्रीरामकृष्ण देव की आत्म-शक्ति की ध्वनि द्वारा निर्मित आपके नाम की ध्वनि की को शास्त्रों में अनाहत नाद के रूप में घोषित किया गया है, जो कूर्म और वायव्य में शक्ति के रूप में विद्यमान है। आप ही तीनो ऐषणा रूपी पाश (या सांसारिक आसक्ति रूपी बंधनकारी रस्सी जो प्राणियों को मृत्यु की तरफ खींचती हैं) को काट देने वाली माँ सारदा के रूप में जानी जाती हैं, इसलिए हे सभी की माँ सारदा, और मुक्ति-भक्ति देने में समर्थ माता कृपया मेरी भी रक्षा करें।
त्वं ब्रह्मपुच्छा विविधा मयूरी, ब्रह्मप्रतिष्ठास्युपदिष्टगीता ।
ज्ञानस्वरूपात्मतयाखिलानां,मां पाहि सर्वेश्वरि मोक्षदात्रि ॥ ५॥
हे मयूरी (माँ श्री सरदा देवी) ! 'ब्रह्म' ( भगवान श्री रामकृष्ण रूपी मयूर) तक पहुँचने के मार्ग (the route to Brahman-Swami Vivekananda) के रूप में, आपकी स्तुति की जाती है। भगवद् गीता द्वारा स्थापित ब्रह्म के रूप में भी आप ही हैं, आप मूर्तमान प्रज्ञा (wisdom personified) हैं, सृष्टि के खेल (सुख-दुःख, बंधन-मुक्ति) का कानून बनाने वाली जगन्माता आप ही हैं। हे मोक्ष-दात्री माता , सबकी माँ सारदा, कृपया मेरी रक्षा करें।
कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जिस सुन्दरता और स्पष्टता से यह उपनिषद् ब्रह्माण्ड के गूढ़ प्रश्नों का उत्तर देता है, और मोक्ष का मार्ग बताता है, उतना सम्भवतः किसी भी उपनिषद् में नहीं दिया गया है । उपनिषदों में श्वेताश्वतरोपनिषद् एक अनपरखा रत्न है !
ब्रह्मचक्र (The Cycle of Creation) साभार -@ https://www.anandamarga.org/articles/brahmacakra/
के चित्र को देखने पर हम देख सकते हैं कि यह चक्र गोलाकार न होकर अंडाकार (oval-shaped ) है।
ब्रह्मचक्र (The Cycle of Creation)
>>>पातंजल योग सूत्र:
जीवन के गूढ़तम् रहस्यों को ज्ञात करने के लिये तथा मनुष्य जीवन को सार्थक करने के लिये, आध्यात्मिक ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। अध्यात्म विज्ञान (मनःसंयोग या ब्रह्मविद्या) से मनुष्य को जीवन के उन गूढ़ रहस्यों का ज्ञान प्राप्त होता है जिसके माध्यम से मनुष्य, जीवन की जटिलतम् समस्याओं (जैसे मृत्यु भय) और परिस्थितियों का समाधान करने की योग्यता प्राप्त करता है। आधुनिक समय में जीवन के रहस्यों को समझने और अध्यात्म से सम्बन्धित विद्याओं को दार्शनिक और काल्पनिक कहकर नकार देने का प्रचलन बढ़ चला है। आज के वैज्ञानिक युग में यदि जन साधारण के समक्ष अध्यात्म की वैज्ञानिक प्रक्रिया (मनःसंयोग आदि 3H विकास के 5 अभ्यास के प्रशिक्षण) को " स्वामी विवेकानन्द -कैप्टन सेवियर वेदान्त शिक्षक -प्रशिक्षण परम्परा -Be and Make ' में प्रशिक्षित एवं चपरास प्राप्त नेता (जीवनमुक्त शिक्षक) के माध्यम से युवा-प्रशिक्षण शिविर का आयोजन व्यापक तौर से किया जाये, तो अध्यात्म के संदर्भ में जो विभिन्न नकारात्मक एवं मिथ्या बातें समाज में प्रचारित हैं उसे आम युवा स्वयं एक परीक्षित सत्य का अनुभव करने के बाद भ्रम समझना बन्द कर देगा ।
>>>योगी किसे कहते हैं ?
योगांग-अभ्यास (मनःसंयोग) द्वारा जब वृत्तिनिरोध वस्तुतः होता रहता है तथा योगज प्रज्ञा (विवेकज ज्ञान) प्रकटित होती रहती है, तब साधक योगी कहलाता है। योगपरम्परा में योगियों के चार भेद (उत्कर्षक्रम के अनुसार) स्वीकृत हुए हैं- कल्पिक, मधुभूमिक, प्रज्ञाज्योतिः तथा अतिक्रान्तभावनीय (द्र. व्यासभाष्य 3/51)। सर्वोच्च स्तर के योगी को अतिक्रान्तभावनीय कहते हैं। ऐसे योगी में कुछ भी भावनीय (अर्थात् विचारणीय एवं संपादनीय) नहीं रह जाता। यह छिन्नसंशय, एवं हृदयग्रन्थिभेदकारी होता है। इसमें प्रान्तभूमि प्रज्ञा पूर्णतः रहती है, अतः इसका कर्म निवृत्त हो जाता है। स्वचित्त को चिरकाल के लिए प्रलीन करना (अर्थात् पुनरुत्थानशून्य करना) ही इनका अवशिष्ट कार्य रहता है। यही जीवन्मुक्त अवस्था है। अतः ऐसे योगी का वर्तमान देह ही अन्तिम देह होता है। (द्र. योगसूत्र 3/51 की भाष्य टीकायें)।
>>>जिसके माध्यम से चित्तवृत्ति का निरोध हो जाता है और मन को आत्मा से योग किया जाता है, और वे इन्द्रिय क्या हैं ?
बाह्य एवं आन्तरविषयों से व्यवहार करने के लिए बुद्धि को जिन साधनों (कारणों) की आवश्यकता होती है, वे इन्द्रिय कहलाते हैं। विषय के द्वैविध्य होने के कारण (या सत्य के duplex-दुतरफा होने के कारण) इन्द्रिय भी द्विविध हैं - आन्तर इन्द्रिय (अर्थात् मन) और बाह्य इन्द्रिय जो ज्ञानेन्द्रिय (sense organs) एवं कर्मेन्द्रिय (sensory organs) के नाम से द्विधा विभक्त हैं। ज्ञानेन्द्रिय का व्यापार है - विषयप्रकाशन और कर्मेन्द्रिय का व्यापार है - विषयों का स्वेच्छया चालन (voluntary movement)। (द्र. ज्ञानेन्द्रिय तथा कर्मेन्द्रिय शब्द)। स्वरूपतः (By nature) इन्दियाँ पंचभूतों द्वारा निर्मित या पंच-भौतिक पदार्थ नहीं हैं (अर्थात् शारीरिक यन्त्र रूप) नहीं हैं - ये अभौतिक पदार्थ हैं - अहंकार से उत्पन्न होने के कारण आहंकारिक-यंत्र कहलाती हैं। स्थूल अंग-विशेष इन्द्रियों (आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा) के (मस्तिष्क में स्थित स्नायु केन्द्र मात्र) अधिष्ठानमात्र हैं।
>>>इन्द्रिय-प्रवृत्ति :- आन्तर इन्द्रिय तथा बाह्य इन्द्रियों की जो प्रवृत्ति (propensity -अपने-अपने विषयों में) होती हैं, वह क्रमशः (respectively) भी होती है, युगपद् (simultaneous) भी। तात्पर्य यह है कि ज्ञानेन्द्रिय की वृत्ति में इन्द्रिय के साथ-साथ मन, अहंकार एवं बुद्धि के भी व्यापार होते हैं। उदाहरणार्थ दर्शन क्रिया कैसे होती है ? रूप के ज्ञान में चक्षुरूप ज्ञानेन्द्रिय के साथ उपर्युक्त तीन अंतःकरण के संकल्प, अभिमान एवं अध्यवसाय रूप व्यापार भी होते हैं। ये चार कभी-कभी युगपद् होते हैं (जैसा कि व्याघ्रदर्शनमात्र से पलायन करना) और कभी-कभी क्रमशः (जैसा कि मन्द आलोक में किसी पदार्थ को यह समझकर कि यह डकैत है, अतः यह हत्या करेगा, यह समझकर पलायन करना)।[(द्र. सांख्यकारिका 30; सांख्यसूत्र 2/32) उपासना/ विश्वनाथ लाल 'शैदा'/https://www.facebook.com/profile.php?id=100067687136822। ]
तत्त्वमस्यादिवाक्येन स्वात्मा हि प्रतिपादितः।
नेति नेति श्रुतिर्ब्रूयादनृतं पाञ्चभौतिकम् ॥
(अवधूत गीता या दत्तात्रेय गीता /१.२५॥)
अर्थ : 'तत्वमसि' आदि वाक्य के द्वारा अपनी आत्मा का ही प्रतिपादन किया गया है। असत्य, जो पांच अवयवों से बना है, उसके बारे में श्रुति कहती है- नेति नेति (यह नहीं, यह नहीं)।
सर्परज्जु में अन्तर लेकिन , विभ्रम की गति न्यारी,
मृग मरीचिका धोखा देती, बनकर जल अनुहारी।
माया- छाया का रहस्य, यदि मर्मी समझ न पाए ,
तो वह संसृति का क्यों कैसे जग को मर्म बताये।।
' नेति नेति ' विचार-पद्धति को वेदान्त का ज्ञानमार्ग कहा जाता है। यहाँ पर ईश्वर का अस्तित्व अन्धविश्वास के ऊपर प्रतिष्टित नहीं है।अद्वैत-वाद में युक्ति-तर्क की सहायता से एक परम-सत्य तक पहुँचना होता है। यह मार्ग चरम विवेक-विचार के उपर प्रतिष्ठित है।इस पथ में युक्ति-तर्क के आधार पर यह सिद्ध किया जाता है कि - ' ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या '। ' नेति नेति ' करते हुए आत्मा की उपलब्धि करने का नाम ज्ञान है। पहले ' नेति नेति ' विचार करना पड़ता है। ईश्वर पंचभूत नहीं है, इन्द्रिय नहीं हैं, मन, बुद्धि, अहंकार नहीं हैं, वे सभी तत्वों के अतीत हैं। रज्जु सर्प उदाहरण में पंचीकरण सिद्धांत के अनुसार रज्जु में सांप का अशं भी मौजूद है,किंतु रज्जु में सांप के अंश की तुलना मे, उसका अपना अंश ही अधिका होत है इसी कारण इस को रस्सी कहा तथा देखा जाता है। अतः यदि रज्जु मे सांप की प्रतीति हुई है तो यह भ्रम अपूर्ण परन्तु सत्य ज्ञान है।
कामवासना कोई पाप तो नहीं ।अगर पाप होती तो तुम न होते । पाप होती तो ऋषि-मुनि न होते ।पाप होती तो बुध्द महावीर न होते ।पाप से बुध्द और महावीर कैसे पैदा हो सकते हैं ?पाप से कृष्ण और कबीर कैसे पैदा हो सकते हैं ?कामवासना तो जीवन का स्त्रोत है । उससे ही लडो़गे तो आत्मघाती हो जाओगे । लडो़ मत , समझो । भागो मत , जागो । कामवासना का पहला काम है तुम्हें जीवन देना और दूसरा काम है तुम्हें जीवन के स्त्रोत से परिचित करा देना । निष्पक्ष भाव से समझने की कोशिश करो , यह कामवासना क्या है । इसके साक्षी बनो ।और जिस दिन तुम पूरे साक्षी हो जाओगे , चमत्कार घटित होता है : कामवासना तिरोहित हो जाती है ।फिर तुम लाना भी चाहो तो नहीं ला सकते ।लडो़ मत । लडा़ई अति है ।एक अति है कामुक व्यक्ति की , जो चौबीस घंटे कामवासना में डूबा हुआ है ; दूसरी अति है ब्रह्मचारी की कि चौबीस घंटे लड़ रहा है । मगर दोनों का केन्द्र कामवासना है ।कामवासना बडा़ रहस्य है जीवन का , सबसे बडा़ रहस्य ।उसके पार बस एक ही रहस्य है --- परमात्मा का ।-- ओशो !
>>>इन्द्रियवध- सांख्य शास्त्र में जो चार प्रकार का प्रत्ययसर्ग माना गया है, उसमें अशक्ति नामक सर्ग के साथ इन्द्रियवध का सम्बन्ध है। अजिघ्रता (नासिका की अशक्ति), वस्तुतः ये अशक्तियाँ बुद्धि की हैं; बुद्धि का अध्यवसाय इन इन्द्रियदोषों के कारण कुंठित हो जाता है।
>>ईश्वर प्रणिधान- ईश्वर को परम गुरु के रूप में समझकर उनमें सब कर्मों का अर्पण करना तथा कर्मफल का त्याग करना ही ईश्वर-प्रणिधान है। (द्र. व्यासभाष्य 2/1, 2/32)।सांख्य-योग दर्शन
>>ऊर्ध्वरेता- शारीरिक शुक्र (वीर्य) की अधोगति जिस योगी में चिरकाल के लिए रूद्ध हो जाती है - कभी भी किसी भी प्रकार से जब शुक्र का स्खलन नहीं होता तब वह योगी ऊर्ध्वरेता कहलाता है। वीर्य या रेतस् ऊर्ध्वगामी होकर ओजस् रूप से परिणत हो जाता है। योगियों की तरह देवजाति-विशेष भी ऊर्ध्वरेता होती है, यह व्यासभाष्य (3/26) में कहा गया है।
>>ऋत-सत्य-ऋत और सत्य ये दोनों ही शब्द धर्म के वाचक हैं। इनमें प्रमात्मक ज्ञान का विषय जो धर्म है, वह ऋत कहलाता है तथा अनुष्ठान का विषय जो धर्म है, वह सत्य कहलाता है। तात्पर्यतः आत्मादि तत्त्व ऋत हैं तथा यज्ञादि कर्म सत्य हैं। अर्थात् ज्ञायमान तत्त्व ऋत है और अनुष्ठीयमान तत्त्व सत्य है (अ. भा. पृ. 206)।वल्लभ वेदांत दर्शन
>>कर्ता : सांख्यीय दृष्टि में कर्तृत्व त्रिगुण में ही रहता है, गुणातीत पुरुष कर्ता नहीं हो सकते। 'त्रिषु गुणेषु कर्तृषु' (तीन गुणों के कर्त्ता होने के कारण) कहा गया है। त्रिगुण में ही कर्तृत्व रहने के कारण पुरुष 'अकर्ता' कहलाते हैं
>>>चित्त क्या है ? ज्ञानानुभूति के साधन को चित्त कहा जाता हैं। महर्षि पतंजलि ने योगदर्शन में मन, बुद्धि, अहंकार इन तीनों के सम्मिलित रूप को चित्त कहा जाता हैं। चित्त शब्द की निरूक्ति 'चित्ति संज्ञाने' धातु से हुयी है। अर्थात् ज्ञानानुभूति का साधन चित्त कहलाता है। चित्त को अन्तः करण या अन्तरिन्द्रिय कहा जाता है। अद्दैत वेदान्त में अन्तःकरण के चार भेद स्वीकार किये गये हैं. मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त।
>>>चित्त का स्वरूप- चित्त का स्वरूप अत्यन्त विलक्षण है। यद्यपि चित्त आत्मा से भिन्न तत्व है फिर भी आत्मा से पृथक करके इसको देखना अत्यन्त कठिन है। चित्त प्रकृति का सात्विक परिणाम है। अतः प्रकृति का कार्य है। प्रकृति त्रिगुणात्मक है। अतः चित्त भी त्रिगुणात्मक है। सत्व की प्रधानता होने के कारण इसको प्रकृति का प्रथम परिणाम माना जाता है। सांख्य और योग के मत में चित् चिति, चैतन्य पुरुष और आत्मा ये सब पर्यायवाचक शब्द हैं। चित्त अपने आप में अपरिणामी, कूटस्थ और निष्क्रिय है। इसी चित्त अथवा पुरुष तत्व को भोग और मोक्ष देने के लिए इसके साथ प्रकृति का संयोग होता है। प्रकृति का प्रथम परिणाम रूप बुद्धि या चित्त तत्व ही भोग और मोक्षरूप प्रयोजन की सिद्धि करता है।
शास्त्रों में चित्त को स्वच्छ दर्पण के समान या शुद्ध स्फटिक मणि के समान बताया है। जैसे ये दोनों सम्पर्क में आने वाले विषयों के आकार को ग्रहण कर तदाकार हो जाते हैं, उन्हीं के रूप रंग को धारण कर लेते हैं। उसी प्रकार चित्त भी जब इन्द्रियों के माध्यम से विषयों के सम्पर्क में आता है तो वह भी उसी विषय के आकार को ग्रहण कर लेता है। जिसे चित्त का विषयाकार होना या चित्त का परिणाम कहा जाता है।
चेतनवत् होते ही चित्त में कार्य करने की क्षमता आ जाती है। चित्त के सम्पर्क से पुरुष में यह परिवर्तन आ जाता है कि वह चित्त के किये गये कार्यों को अपना कार्य मान बैठता है। जो कर्तृत्व और भोक्तृत्व चित्त का धर्म था, अहंकारवश पुरुष स्वयं को कर्ता और भोक्ता मान बैठता है। रत्नमाला शास्त्र में बताया गया है कि जिस क्षण गुरु निर्विकल्प स्वरूप को प्रकाशित कर देते हैं, तभी शिष्य मिथ्या अहंकार से मुक्त हो जाता है।
>> चित्तभूमि- जो अवस्था (धर्मविशेष) चित्त में अनायास उदित रहती है, वह भूमि कहलाती है। चित्त में प्रकृति के तीनों गुण सत्व, रज और तम विद्यमान हैं। सबके चित्त एक समान नहीं हैं। व इन तीनों की विभिन्न स्थितियों के कारण चित्त भी विभिन्न स्थितियों वाला हो जाता है। जिन्हें चित्त की अवस्थायें या चित्तभूमि के नाम से भी जाना जाता है। योगदर्शन में चित्त की स्थितियों को मूढ, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध इन पाँच स्थितियों में बॉटा है। प्रत्येक भूमि में समाधि हो सकती है, अतः समाधि को 'चित्त का सार्वभौम धर्म' कहा जाता है।
>>चैतन्य : 'चैतन्यलक्षणः पुरुषः' आदि शास्त्रवाक्यों में चैतन्य तथा 'पुरुष' एक ही पदार्थ हैं - लक्षण को स्वरूप मानकर ऐसा प्रयोग किया गया है।सांख्ययोगशास्त्र में 'चैतन्य' और 'चेतन' समानार्थक हैं। दोनों शब्द चित्-स्वरूप पुरुष के वाचक हैं। 'चेतन का भाव' - इस अर्थ में चैतन्य शब्द इस शास्त्र में प्रयुक्त नहीं होता। चैतन्य वह सारतत्त्व है जिसके कारण वस्तु चेतन होती है। अतएव हर एक भाव की आत्मा, अर्थात् उसकी भावता का मूल-आधार, चैतन्य होता है। समस्त प्रमेय जगत् का वास्तविक स्वरूप यह चैतन्य ही है। (शि.सू.वा.पृ. 3)।
>>>जप -मन्त्र की पुनः पुनः आवृत्ति, उसका बार-बार उच्चारण जप कहलाता है। मन्त्र का जप करते समय उसके अर्थ की भी भावना करनी चाहिये। ऐसा करने से मन्त्रवीर्य, मन्त्रचैतन्य का आविर्भाव शीघ्र होता है। अपने इष्टदेव से तादात्म्य स्थापित करने के लिए मंत्र -'I am He' के बारबार दोहराए जाने को जप कहते हैं। गुरुमुख से प्राप्त मन्त्र का जप ही फलदायक होता है। पुस्तक में लिखे मन्त्र का जप करने से कोई सिद्धि नहीं मिलता। स्वप्नलब्ध मन्त्र का जप भी सिद्धिकर माना गया है। शाक्त दर्शन। जप तीन प्रकार का होता है - मानस, उपांशु और वाचिक । मन्त्रार्थ का विचार करते हुए उसकी मन ही मन आवृत्ति करना मानस जप है। देवता का चिन्तन करते हुए जिह्वा और दोनों होठों को थोड़ा हिलाते हुए किंचित् श्रवण योग्य जप उपांशु कहलाता है। जो दूसरे व्यक्ति को भी स्पष्ट सुनाई पड़े, ऐसा उच्च स्वर से किया गया जप वाचिक कहलाता है। वाचिक से उपांशु दस गुना और मानस जप सहस्त्र गुना फल देने वाला है। जप की सिद्धि हो जाने पर मन्त्र में चैतन्य का आविर्भाव होता है और ऐसा होने पर साधक उसकी सहायता से अनायास सिद्धि लाभ कर सकता है।
>>जीव अवस्था-त्रय : सच्चिदानंदात्मक अणु रूप शुद्धावस्था नित्यमुक्त अवस्था (नारद-शुकदेव की अवस्था) है। बद्ध, मुमुक्षु, मुक्त जीव की तीन अवस्थायें हैं। अविद्या से बद्ध और दुःखित अवस्था जीव की संसारी अवस्था है। देहाध्यास, इन्द्रियाध्यास, प्राणाध्यास, अन्तःकरणाध्यास तथा स्वरूप विस्मृति ये ही अविद्या के पाँच पर्व हैं। जन्म-मरण आदि संसारी धर्मों का अनुभव करता हुआ भी भगवत् कृपा से प्राप्त सत्संग द्वारा पंच पर्वात्मक विद्या पाकर परमानंद स्वरूप मुक्ति जीव की मुक्तावस्था है। वैराग्य, ज्ञान, योग, तप और केशव में भक्ति ये ही विद्या के पाँच पर्व हैं। (वल्लभ वेदांत दर्शन)
>>>जीवन्मुक्त : धर्ममेघसमाधि के द्वारा क्लेश और कर्मों की निवृत्ति होने पर ही कोई व्यक्ति जीवन्मुक्त होता है। इस अवस्था में क्लेश की स्थिति 'दग्धबीजवत्' हो जाती है, अर्थात् जीवन्मुक्त क्लेश के अधीन होकर कोई कर्म नहीं करते। नूतन विपाक को उत्पन्न करने में कर्माशय असमर्थ हो जाता है, केवल प्रारब्ध कर्म का भोग होता रहता है और योगी अनासक्त होकर इस भोग का अनुभव करते रहते हैं (द्र. योगसू. 4/30)। जीवन्मुक्त अवस्था कैवल्यप्राप्ति की पूर्वावस्था है। वह समस्त विश्व को तथा इसके समस्त व्यवहार को एक नाटक के दृश्य के तुल्य मानता है, अथवा इसे अपनी ही (माता के) परिपूर्ण शक्ति का विलास समझता है। इस प्रकार वह समस्त सांसारिक व्यवहारों को करता हुआ भी उनसे मुक्त ही बना रहता है। यह ज्ञानी-भक्त की जीवन्मुक्ति होती है। जीवन्मुक्त का स्वेच्छासाध्य मुख्य कर्म है - मोक्ष विद्या (मनुष्य-निर्माण और चरित्रनिर्माणकारी शिक्षा) का उपदेश जिसको वे निर्माणचित्त का आश्रय करके करते हैं। जीवन्मुक्ति के बाद पुनः संसारबन्धन नहीं हो सकता। इस अवस्था के बाद विदेहमुक्ति (शरीरत्यागपूर्वक कैवल्यप्राप्ति) होने में कुछ काल लगता है जो अवश्यंभावी है। इस काल की उपमा कुम्भकार -चक्र का भ्रमण है। नूतन वेग-कारक क्रिया न करने पर भी प्राक्तन वेग के संस्कार से जिस प्रकार चक्र कुछ काल तक घूमता रहता है, उसी प्रकार देहधारण -संस्कार के कारण नूतन कर्म संकल्प से शून्य जीवन्मुक्त का शरीर कुछ काल के लिए जीवित रहता है।
>>तत्त्वसर्ग = तत्त्वों का सर्ग = सृष्टि। तत्त्व = महत - अहंकार - तन्मात्र - इन्द्रिय - मन - भूत। इन तत्त्वों के मूल उपादान अव्यक्त (साम्यावस्था प्राप्त त्रिगुण) हैं और मूल निमित्त अपरिणामी चेतन पुरुष है। इन तत्त्वों की सृष्टि का क्रम नियत है। क्रम यह है - प्रकृति से महत्तत्त्व, महत् से अहंकार, अहंकार के सात्त्विक भाग से दस इन्द्रियाँ तथा मन एवं उसके तामस भाग से पाँच तन्मात्र; पाँच तन्मात्रों से पाँच भूत।
>>त्रिकोण बीज - इसमें इच्छा, ज्ञान एवं क्रिया नामक तीन शक्तियाँ समरस अवस्था में ही रहती हैं। (शि.सू.वि.पृ. 30)। इसको इसलिए भी त्रिकोण बीज कहते हैं कि प्राचीन शारदा लिपि में इसका आकार एक ओर से त्रिकोणात्मक ही होता था। त्रिकोण जैसे आकार के कारण इसका नाम योनिबीज भी है।काश्मीर शैव दर्शन
>>दग्धबीजवद्भाव-अस्मिता, रोग, द्वेष और अभिनिवेश नामक क्लेशों की चार प्रसिद्ध अवस्थाएँ हैं -प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार (योगसूत्र 2/4)। इन चारों के अतिरिक्त एक पाँचवी अवस्था भी है, जो प्रसुप्त अवस्था (क्लेशों का शक्ति रूप में रहना, जिससे उचित अवलम्बन मिलने पर वे सक्रिय होकर कर्म को प्रभावित करते हैं) से भी सूक्ष्म तथा उससे विलक्षण स्वभाव की है। यह पाँचवीं अवस्था दग्धबीजावस्था कहलाती है। इस अवस्था में आलम्बन के साथ संयोग होने पर भी क्लेश सर्वथा निष्क्रिय ही रहता है। दग्धबीज की उपमा से यह भी ध्वनित होता है कि जिस प्रकार जले बीज का बाह्य आकार मात्र रह जाता है, इसी प्रकार इस अवस्था में भी बाह्यदृष्टि से ऐसा प्रतीत होता है कि योगी का कर्म क्लेशपूर्वक हो रहा है - पर वस्तुतः ऐसा नहीं होता।सांख्य-योग दर्शन
>>दृश्य-जगत : योगसूत्र (2/17; 2/18) के अनुसार दृश्य-जगत त्रिगुण की व्यक्तावस्था है। चूंकि द्रष्टा से संयुक्त होने पर अव्यक्त त्रिगुण व्यक्त होता है, अतः दृश्य (अर्थात् द्रष्टा का जो दृश्य होगा, वह) व्यक्त त्रिगुण होगा। अतः दृश्य का अर्थ 'महत्तत्त्व से शुरु कर भूतपर्यन्त सभी पदार्थ' है। अव्यक्त प्रकृति के लिए यदि 'दृश्य' का प्रयोग हो तो वहाँ दृश्य का अर्थ 'द्रष्टा के द्वारा प्रकाशित होने योग्य' होगा।(सांख्य-योग दर्शन)
>>>देव (श्रीरामकृष्ण देव) : ईश्वर का नामांतर। पाशुपत शास्त्र में ईश्वर का नाम देव भी आया है। देव शब्द 'दिवु क्रीड़ायाम्' से बना है। ईश्वर स्वभावत: क्रीड़नशील है। वह अपने स्वतंत्र क्रीड़नशील स्वभाव के कारण ही कार्य की उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार करता है, अतः देव कहलाता है। इस तरह से यह जगत उसकी क्रीड़ा का प्रसार है। यह सत्य है। मिथ्या नहीं है। इस जगत में प्रत्येक पदार्थ जो प्रकट होता है वह शिव की ही लीला से प्रकट होता है। अनादि अविद्या से प्रकट नहीं होता। तो पाशुपत दर्शन परमैश्वर्य सिद्धांत का पोषक है, विवर्तवाद का पोषक नहीं है। (पा.सू.कौ.भा.पृ.56)। शिव की ऐसी लीलामय शक्ति ही उसका देवत्व कहलाती है। (पाशुपत शैव दर्शन)
>>>देशबन्ध>चित्त का देशबन्ध धारणा है - यह योगसूत्र (3/1) का मत है। ध्येय की चिन्ता करना किसी देश में ही संभव होता है, इसलिए धारणा को 'देशबन्ध' कहा जाता है। देश दो प्रकार का है - बाह्य तथा आभ्यन्तर। आभ्यन्तर देश आध्यात्मिक देश कहलाता है, जो शरीर के अन्तर्गत विशिष्ट स्थान प्रधानतः मर्म स्थान हैं। नाभि, हृदय, मूर्छा, नासिकाग्र, जिह्वाग्र, तालु, वक्ष, मुख, कण्ठ, भ्रूमध्य, नेत्र आदि प्रसिद्ध आध्यात्मिक देश हैं। सूर्य, चन्द्र, अग्नि या देवमूर्ति-विशेष (ठाकुर, माँ , स्वामीजी?) बाह्य देश हैं। इन देशों के साथ चित्त का बन्धन ज्ञान या वृत्ति के माध्यम से किया जाता है। सांख्य-योग दर्शन
>>>देह> देह वह भूतनिर्मित वस्तु है, जो लिंग (सूक्ष्म शरीर) का आश्रय है। इस देह रूप आश्रय के बिना लिंग सक्रिय रहकर भोग-अपवर्ग का साधन नहीं कर सकता। देह का विभाग नाना दृष्टियों से सांख्ययोगशास्त्र में किया गया है, जैसे योनिज-अयोनिज देह। कोई-कोई भोगदेह-कर्मदेह-उभयदेह रूप भेद को मानते हैं (सांख्यसू. 5/124)। जिस शरीर में स्वेच्छया पुरुषकारपूर्वक कर्म करना अधिक मात्रा में संभव है, वह कर्मदेह है; भोग का भोगना ही जिस देह में प्रधान रूप में होता है, वह उपभोग देह या भोगदेह है; जिसमें भोग और कर्म दोनों ही समभाव में हो सकते हैं - वह उभयदेह है। देवयोनि, तिर्यक्योनि एवं मनुष्ययोनि रूप त्रिविध जीवों के तीन प्रकार की देह की अपनी विशिष्टता है। (इस विशिष्टता के विवरण के लिए देवल के वचन द्रष्टव्य; ये वचन कृत्यकल्पतरु, मोक्षकाण्ड, पृ. 109 में उद्धृत हैं)। (सांख्य-योग दर्शन)
>>>दोष >पतंजलि कहते हैं कि दोष-बीज का क्षय होने पर कैवल्य होता है (योगसूत्र 3/50)। व्याख्याकारों ने दोष का अर्थ क्लेश (अविद्या आदि) किया है, जो संगत प्रतीत होता है। `दोष के कारण ही मोक्षमार्ग पर शंका होती है` (4/25 व्यासभाष्य में उद्धृत) - इस पूर्वाचार्यवचन में भी दोष का अर्थ अस्मितारागादि क्लेश ही हैं। अशुद्धि -अर्थ में दोष शब्द प्रायः प्रयुक्त होता है, जैसे विषयदोष (विषय में रहने वाला दोष जिससे वह मन को चंचल करता है), संगदोष (अनभीष्ट वस्तु या व्यक्ति के साथ संसर्ग जो चित्त को एकाग्र नहीं होने देता) आदि शब्द इस अर्थ के उदाहरण हैं। आयुर्वेद के वात -पित्त -कफ को दोष कहा जाता है; योगग्रन्थों में भी ऐसा कथन उपलब्ध होता है (व्यासभाष्य 3/29)।सांख्य-योग दर्शन
>>>द्रष्टा>बुद्धि के साक्षीभूत जो पुरुष (तत्त्व) हैं; वे 'द्रष्टा' कहलाते हैं। ये अपरिणामी कूटस्थ एवं निर्धर्मक हैं। दृश्य (बुद्धि) की अपेक्षा से ही पुरुष द्रष्टा कहलाते हैं। दृश्य सम्बन्धहीन पुरुष के लिए भी द्रष्टा शब्द प्रयुक्त होता है, यद्यपि यहाँ 'चित्त', 'चित्ति' आदि शब्द अधिक संगत हैं। 'द्रष्टा' का शब्दार्थ यद्यपि 'दर्शनक्रिया का कर्त्ता' है, तथापि पुरुष-रूप द्रष्टा में किसी भी प्रकार का कर्तृत्व नहीं है। सर्वविशेषणशून्य, विषयहीन, परिणामहीन ज्ञातामात्र द्रष्टा है। क्रियाकारकशून्यता को दिखाने के लिए ही योगसूत्रकार ने द्रष्टा के लक्षण में 'दृशिमात्र' शब्द का प्रयोग किया है (2/20)। इस द्रष्टा के योग से ही अचेतन त्रिगुणजात बुद्धि चेतन-सी होती है और भोग-अपवर्ग का साधन करती रहती है। योगसूत्र 2/20 में द्रष्टा को प्रत्ययानुपश्य कहा गया है, अर्थात् परिणामी बुद्धिवृत्ति में प्रतिबिम्बित होकर वह वृत्तिसाक्षी के रूप में रहता है, वृत्तियों के आकार में परिणत नहीं होता (जैसे चित्त एवं उसकी वृत्तियाँ स्व-स्व विषयाकार से आकारित होती हैं)। बुद्धि का द्रष्टा होने के कारण ही अविवेकियों को पुरुष द्रष्टा -सदृश प्रतीत होता है और यह भ्रम ही बन्धन का हेतु है।सांख्य-योग दर्शन
>>>द्वादशान्त > प्राणशक्ति के उदय एवं विश्रांति का स्थान। (तं.आ.वि. 4 पृ. 157)। द्वादशांत आंतर अपान नामक प्राण का नासिका छिद्र से बारह अंगुल भीतर हृदय में विश्रांति का स्थान। साधना के क्रम में इस विश्रांति के क्षण में शून्य भाव की भावना की जाती है। (वि.भै.51)। द्वादशांत उर्ध्व प्राणशक्ति का ब्रह्मरंध्र से बारह अंगुल ऊपर विश्रांति का स्थान। (वि.भै. 22)। इसकी अनुभूति योगियों को ही होती है। द्वादशांत बाह्य नासिका छिद्र से बारह अंगुल बाहर प्राणवायु का विश्रांति स्थान।काश्मीर शैव दर्शन
प्राण और अपान की गति की जिस स्थान पर उत्पत्ति होती है, अथवा जाकर जहाँ रुक जाती है, उसको हृदय और द्वादशान्त कहते हैं। बाह्य और आन्तर शिव द्वादशान्त और शक्ति द्वादशान्त के भेद से द्वादशान्त की द्विविध स्थिति मानी गई है। द्वादशान्त पद की व्याख्या करते हुए शिवोपाध्याय (विज्ञान भैरव. पृ. 43) कहते हैं कि शरीर के प्रत्येक रोमकूप में द्वादशान्त की स्थिति है। यहाँ द्वादशान्त पद का प्रयोग लाक्षणिक है। जैसे मुख्य द्वादशान्त की स्थिति द्वादश आधारों के अन्त में है, उसी तरह से सभी नाडियों के अन्त (रोमकूप) में भी प्राण शक्ति की स्थिति है।
'हकार' की उत्पत्ति हृदय में और 'सकार' की उत्पत्ति द्वादशान्त में मानी जाती है। हृदय स्थित कमलकोश में प्राण का उदय होता है। नासिका मार्ग से बाहर निकल कर यह बारह अंगुल चलकर अन्त में आकाश में विलीन हो जाता है। इसीलिये बाह्य आकाश योगशास्त्र में द्वादशान्त के नाम से प्रसिद्ध है। शिखा के अन्त में उन्मना शक्ति का निवास है। इस प्रकार द्वादशान्त की स्थिति ब्रह्मरन्ध्र से पृथक मानी गई है। इसको द्वादशान्त इसलिये कहते हैं कि द्वादश आधारों के अन्त में इसकी स्थिति है। निर्विकल्प महायोगी द्वादशान्त के भी ऊपर स्थित परमाकाश में जब पहुँच जाता है, तो उस स्थिति में सर्वात्मता का विकास होने से वह अनुत्तर शून्य में लीन हो जाता है। योगिनीहृदय (1/27, 34) में इसको महाबिन्दु कहा गया है। वहाँ आज्ञाचक्र तक की स्थिति को सकल, उन्मना पर्यन्त स्थिति को सकल-निष्कल और महाबिन्दु को निष्कल माना गया है। इस निष्कल स्वरूप में भगवती त्रिपुरसुन्दरी निवास करती है। (शाक्त दर्शन)
>>>द्वैताद्वैतात्मक-विशेषाद्वैत> वीरशैव दर्शन के अनेक नामों में यह भी एक नाम है। इस नाम से वीरशैव-सिद्धांत का प्रतिपाद्य विषय ज्ञात होता है। 'वि:' शब्द का पक्षी और परमात्मा, ये दो अर्थ होते हैं। 'द्वासुपर्ण सयुजा सखाया --- अभिचाकशीति' (मु. 3-1-1)' इस मंत्र में शिव का पक्षी के रूप में वर्णन किया गया है। अतः इस प्रमाण के आधार पर यहाँ 'वि:' शब्द का अर्थ परमात्मा अर्थात् 'शिव' लिया गया है। 'शेष' शब्द का अर्थ होता है 'अंश'। इस प्रकार 'वि:' का अर्थ 'शिव' और 'शेष' का अर्थ 'जीव' है। अतः शिव और जीव इन दोनों का अद्वैत ही 'विशेषाद्वैत' कहलाता है। यहाँ पर शिव और जीव का अद्वैत 'यथा नद्य: स्यंदमाना: समुद्रടस्तं गच्छंति नाम रूपे विहाय ---- तथा ---- पुरुषमुपैतिदिव्यग् (मु. 3-2-8)' इस श्रुति के अनुसार समुद्र और नदी के दृष्टांत से प्रतिपादिप किया गया है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जैसे समुद्र से भिन्न स्वरूपवाली नदियाँ समुद्र से मिलकर समुद्रस्वरूप हो जाती हैं, उसी प्रकार संसार-दशा में वस्तुत: शिव से भिन्न स्वरूप वाला जीव मुक्तावस्था में शिव के साथ सर्वथा अभिन्न अर्थात् समरस हो जाता है। अतः इस दर्शन में शिव और जीव के भेद तथा अभेद इन दोनों को सत्य मानते हैं। द्वैत तथा अद्वैत प्रतिपादक दोनों प्रकार की श्रुतियों का समन्वय करने के लिए इस दर्शन में भेद और अभेद दोनों को सत्य माना गया है। इसीलिये द्वैत श्रुतियों के आधार पर मुक्तावस्था में उन दोनों के अभेद के प्रतिपादक इस दर्शन को 'द्वैताद्वैतात्मक-विशेषाद्वैत' कहते हैं। (श्रीकर. भा. मंगलश्लोक 14,15 पृष्ठ 2)। (वीरशैव दर्शन)
>>>धारणा >धारणा अष्टांग योग का छठा अंग है। किसी बाह्य देश या आध्यात्मिक देश (द्र. 'देशबंध') में चित्त को बाँधना धारणा है (योगसू. 3/1)। जिस चित्तबन्धन में उस देश से अतिरिक्त अन्य किसी देश में चित्त का संचरण नहीं होता है (यह प्रत्याहार के द्वारा ही संभव होता है) वही धारण योगशास्त्रीय धारणा है ('धारणा' शब्द का प्रयोग भावना के अर्थ में भी होता है)। मन को दृढ़रूपेण ध्यान में स्थापित करना। पाशुपत योग के अनुसार हृदय में ओंकार की धारणा करनी होती है। धारणा वह उत्कृष्ट योग है जहाँ आत्म तत्व में लगाए हुए ध्यान को स्थिरता दी जाती है। ध्यान जब दीर्घ काल के लिए साधक के मन में स्थिर रहता है तो वह धारणा कहलाती है।
>>>धर्म>बल का एक प्रकार। पाशुपत शास्त्र में पाशुपत धर्म की निर्धारित विधि - यम-नियम का सदैव पालन करना धर्म कहलाता है। धर्म बल का चतुर्थ भेद है। क्योंकि धर्म पर स्थित होने से बल आता है (ग.का.टी.पृ.7)। धर्म से पूजापाठ आदि प्रसिद्ध लोकप्रिय धर्म तथा यम नियम आदि विशेष साधक धर्म यहाँ अभिप्रेत हैं। इन धार्मिक कृत्यों के अनुष्ठान से चित्त शोधन होता है और उससे साधना सफल होती है। इस तरह से धर्म रूपी बल साधना में सफलता प्राप्त करने में सहायक बनता है।पाशुपत शैव दर्शन
>>>धर्मशक्ति>तप का चतुर्थ लक्षण। पाशुपत दर्शन के अनुसार जिस शक्ति के बल से साधक का योगनिष्ठ चित्त किसी भी बाह्य स्थूल विषय की ओर आकृष्ट न हो, अर्थात् किसी भी प्रकार के मोह से मोहित न हो, वह सामर्थ्य धर्मशक्ति कहलाती है। (ग.का.टी.पृ.15)। इसी शक्ति से योगी काम, क्रोध, लोभ आदि से अस्पृष्ट रहता हुआ स्थिरता से अपने अभ्यास में ही लगा रहता है।पाशुपत शैव दर्शन
>>>धर्ममेघ समाधि योग की एक अवस्था है। जिस समाधि के द्वारा क्लेशों एवं कर्मों की निवृत्ति होती है, वह धर्ममेघसमाधि है। चित्तवृत्ति के निरोध से योग या समाधि होती है। चित्त त्रिगुणात्मक है। ये गुण हैं सत्त्व, रज, और तम। जब सत्त्व गुण का पूर्ण विकास होता है तब चित्त स्वस्वरूप में अवस्थित हो जाता है तथा उसमें विवेकख्याति विषयक समापत्ति (बुद्धि और पुरुष के भेद का ज्ञान) उत्पन्न होती है, और यही अवस्था धर्ममेघ समाधि कही जाती है।
सर्वज्ञता -रूप प्रसंख्यान पर भी जब योगी का वैराग्य होता है, तभी यह समाधि आविर्भूत होती है (योगसू. 4/29)। इस अवस्था में विवेकख्याति की पूर्णता हो जाती है और योगी इस ख्याति को भी निरुद्ध करने के लिए उद्यत हो जाता है। आत्मज्ञान रूप धर्म का ही मेहन (= वर्षण) करने के कारण ही इस समाधि का 'धर्ममेघ' नाम है। योगियों का कहना है कि इस समाधि का लाभ होने पर अनायास कैवल्य की प्राप्ति होती है।(सांख्य-योग दर्शन)
इसका नाम धर्ममेघ इसलिए पड़ा क्योंकि यह आत्मदर्शन रूप परमधर्म (कैवल्य) की वर्षा कर साधक के चित्त को सींचता है। यह साधना की अन्तिम सीमा है। सन्तों ने मेघ बरसने की चर्चा इसी सन्दर्भ में की है। कबीर कहते हैं -
" गगन गरजै बिजुली चमकै, उठती हिए हिलोर।
बिगसत कंवल मेघ बरसाने चितवत प्रभु की ओर।"
पतंजलि ने अपने योगसूत्र में कहा है कि विवेकज ज्ञान में भी विरागयुक्त होने पर सर्वथा विवेकख्याति होने से धर्ममेघ समाधि उत्पन्न होती है। धर्ममेघ समाधि की उपलब्धि व्यक्ति को समस्त क्लेशों से मुक्त कर देता है। इससे सम्यक् निवृत्ति या सम्यक निरोध सिद्ध होता है। इसी को जीवनमुक्ति कहा जाता है।जीवन्मुक्त का स्वेच्छासाध्य मुख्य कर्म है - मोक्ष विद्या का उपदेश जिसको वे निर्माणचित्त का आश्रय करके करते हैं। किसी-किसी का मत है कि जीवन्मुक्त अवस्था में जाति-आयु-भोग रूप त्रिविध विपाकों में केवल आयुविपाक ही सक्रिय रहता है। जीवन्मुक्त अवस्था कैवल्यप्राप्ति की पूर्वावस्था है।
>>>नर तत्त्व>त्रिकशास्त्र की त्रितत्त्व कल्पना में जड़ तत्त्व को नर तत्त्व कहते हैं। नर का अर्थ है मायीय प्रमाता। मायीय प्रमाता या तो स्थूल शरीर को, या प्राण को, या बुद्धि को या शून्य को जाग्रत्, स्वप्न और सुषुप्ति में अपना आप समझता है। ये सभी पदार्थ जड़ हैं। अतः इस मायीय प्रमाता को जड़ तत्त्व में गिनते हुए नर तत्त्व कहा जाता है। यह सारा जड़ जगत् भी नर तत्त्व में ही गिना जाता है। इस तरह से जीव और उसका जगत् नर तत्त्व कहलाता है। (पटलत्री.वि.पृ. 73, 74)।काश्मीर शैव दर्शन
>>>नवमुण्डी और पंचमुण्डी आसन> योगासनों से शरीर की विभिन्न स्थितियों में सुविधाजनक स्थिरता प्राप्त की जाती है, जब कि प्रस्तुत आसनों का उपयोग साधना में बैठते समय स्थिर और सुखदायक आधार के रूप में किया जाता है। कुशासन, कम्बल, गलीचा, अजिन (मृगचर्म), व्याघ्रचर्म आदि आसनों से सभी परिचित हैं, सुखदायक आसन पर बैठकर योगांग आसन का अनायास अभ्यास किया जा सकता है एवं उससे प्राणायाम और चित्त की एकाग्रता सहज सिद्ध हो सकती है। तन्त्रसाधना में पंचमुण्डी आसन बंगदेश में प्रसिद्ध हैं। अवतार वरिष्ठ भगवान श्री रामकृष्ण अपनी लीला में और साधक रामप्रसाद, कमलाकान्त आदि ने अपनी साधना के दौरान पंचमुण्डी आसन पर बैठकर ही सिद्धि प्राप्त की थी। इस समय भी बंगदेश तथा काशी प्रभृति स्थानों में भी किसी न किसी साधक का पंचमुण्डी आसन प्रसिद्ध है। नवमुण्डी आसन का रहस्य अब तक रहस्य ही बना हुआ है। इस नवमुण्डी आसन के आध्यात्मिक रहस्य को समझाने का प्रयत्न स्वयं श्रद्धैयचरण गुरुप्रवर श्री श्री गोपीनाथ कविराज महोदय ने अपने ग्रन्थ 'तान्त्रिकवाङ्मय में शाक्तदृष्टि' के 'श्री श्री नवमुण्डी महासन' शीर्षक निबन्ध (पृ. 261-278) में किया है। जिज्ञासु जनों को इस रहस्य को वहीं समझने का प्रयत्न करना चाहिये।शाक्त दर्शन
>>>नाड़ीत्रय> मेरुदंड में स्थित सुषुम्ना, पिंगला तथा इड़ा नामक तीन नाड़ी स्वरूप मार्ग जिन्हें क्रमशः इच्छा, ज्ञान तथा क्रिया प्रधान माना गया है। इन्हें क्रमशः वह्नि, सूर्य तथा सोमात्मक भी माना जाता है। सुषुम्ना मेरुदंड के मध्य में, पिंगला दाईं ओर तथा इड़ा बाईं ओर स्थित होती है। ये नाडियाँ भी तो धारणा का विषय बनती ही हैं।काश्मीर शैव दर्शन
>>>नाड़ीशुद्धि प्राणायाम> इस प्राणायाम विशेष के अभ्यास से नाडियों में जो शुद्धि होती है, वह नाडीशुद्धि कहलाती है। मल के कारण शरीर योगाभ्यास के लिए समर्थ नहीं होता या अत्यल्प योगाभ्यास से ही कातर हो जाता है। शीत, ग्रीष्म, जल, हवा आदि से अत्यधिक पीड़ित होते रहना भी नाडीगत मल के कारण होता है। विभिन्न प्रकार के प्राणायामों द्वारा नाडीशुद्धि होने पर शरीर रोगहीन, उज्जवलकान्तिमय, लघुतायुक्त, सौम्यदर्शन होता है। नाडी शुद्धिकारक प्राणायामों का विशद विवरण हठयोग के ग्रन्थों में (हठयोगप्रदीपिका, घेरण्डसंहिता आदि में) मिलता है।सांख्य-योग दर्शन
>>>नाद > अव्यक्त ध्वनि। हकारात्मक अवाहत ध्वनि। पर बीज। भ्रूमध्य में अभिव्यक्त होने वाला हंस स्वरूप बीज। नाद वाणी का निर्विकल्पक रूप होता है। हकारात्मक शक्ति को भी नाद कहते हैं। प्रणव उपासनारूपी योग की सातवीं कला को भी नाद कहा जाता है। इस प्रकार से नाद शब्द का प्रयोग शैव शास्त्र में अनेकों अर्थो में हुआ है। नाद का विशेष अर्थ स्वात्म विमर्श है। उसी को इस शास्त्र में शब्द तत्त्व कहा गया है।
त्रिकयोगमयी प्रणव की उपासना में अकार, उकार, मकार, बिंदु, अर्धचंद्र के अनंतर योगियों के साक्षात्कार में अभिव्यक्त होने वाली (प्रणव की) सातवीं कला का नाम भी नाद है। बिंदु का उच्चारण काल आधी मात्रा, अर्धचंद्र का एक चौथाई मात्रा, निरोधी का 1/8 मात्रा और नाद का 1/16 मात्रा होता है। शिवयोगियों की अवधानमयी दृष्टि इतनी पैनी बन जाती है कि प्रणव की ध्वनि की गूंज का इतना सूक्ष्म विश्लेषण कर पाती है।
>>>नाद-बिन्दु > ग्रन्थों में नाद और बिन्दु को शिव और शक्ति से उसी तरह से अभिन्न माना गया है, जैसे कि शब्द और अर्थ को अभिन्न माना गया है। प्रणव की 12 कलाओं में भी बिन्दु और नाद की स्थिति है। नादकारिका (श.र.सं., पृ. 40) में नाद को मालिनी, महामाया, समना, अनाहत बिन्दु, अघोषा वाक् और ब्रह्मकुण्डलिनी बताया है। 'हकारस्तु स्मृतः प्राणः स्वप्रवृत्तो हलाकृतिः' (4/257) स्वच्छन्दतन्त्र के इस वचन के अनुसार स्वाभाविक रूप से निरन्तर नदन करने वाले हलाकृति प्राण को ही हकार कहा गया है। अनच्क हकार की आकृति वाले प्राण का यह नदन व्यापार ही हंसोच्चार कहलाता है। इसी को अनाहत ध्वनि अथवा नादभट्टारक भी कहा जाता है। भट्टारक शब्द अतिशय आदर का सूचक है। दस प्रकार के नाद में धारणा, ध्यान और समाधि का अभ्यास करने पर योगी शब्दब्रह्म के स्वरूप को भली-भांति समझ लेता है। वह यह जान लेता है कि शब्दब्रह्म से ही परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी - इन चार प्रकार की वाणियों का विकास होता है। यह नाद तत्त्व परा और पश्यन्ती के क्रम से विकसित होता हुआ मध्यमा में आकर योगाभ्यास द्वारा श्रवणेन्द्रिय के अन्तर्मुख होने पर सुनाई पड़ता है। अन्तर्मुखता की ओर बढ़ते-बढ़ते, अर्थात् इस नाद के सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम स्वरूप का अन्वेषण करते-करते योगी शब्दब्रह्म के स्वरूप को भली-भांति समझने में समर्थ हो जाता है, निष्णात हो जाता है। इस निरन्तर नदन करती अनाहत ध्वनि में चित्त को एकाग्र कर लेने पर योगी का परमाकाश स्वभाव, चिदाकाशमय प्रकाशात्मक स्वरूप प्रकट हो जाता है।शाक्त दर्शन
>>>नारायण>नार अर्थात् जीव समूह को प्रेरित करने वाला या जीव समूह में प्रविष्ट हुआ परमात्मा नारायण है। अथवा सब कुछ जिसमें प्रविष्ट हो, ऐसा जो जगत का आधार है, वह नारायण है। `नराज्जातानि तत्त्वानि नाराणीति विदुर्बुधाः। तस्य तान्ययनं पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः।। अथवा आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः। तस्य ता अयनं पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः।।वल्लभ वेदांत दर्शन
>>>नित्यात्मा>आत्मतत्व के साथ शाश्वत योग। पाशुपत मत के अनुसार युक्त साधक को आत्मा के साथ निरंतर योग होता है, अर्थात् वह आत्म तत्व के साथ सदैव एकाकार बनकर ही रहता है। सर्वदा चित्तवृत्ति का आत्मतत्व में ही समाधिस्थ होकर रहना नित्यात्मत्व कहलाता है। (अनुरूध्यमान चितवृत्तित्वं नित्यात्मत्वम्- ग.का.टी.पृ. 16)। नित्यात्मत्व अवस्था को प्राप्त साधक नित्यात्मा कहलाता है। (पा.सू.पृ. 5.3)। पाशुपत शैव दर्शन
>>>निरंजन> मुण्डकोपनिषद् (3/1/3) में कहा गया है कि निरंजन परम साम्य को प्राप्त कर लेता है। यहाँ निरंजन पद मुक्त जीव के लिये प्रयुक्त है। पाशुपत मत में पशु (जीव) के दो भेद बताये गये हैं - सांजन और निरंजन। उनमें से शरीर इन्द्रिय आदि से संबद्ध पशु सांजन और इनसे रहित पशु को निरंजन कहा गया है। माया में पड़ा हुआ जीव सांजन और उससे अतीत निरंजन कहा जाता है। शाक्त दर्शन
>>>नेत्रत्रय>भगवान् शिव को त्र्यम्बक कहा जाता है। इनके तीनों नेत्र सदा उन्मीलित रहते हैं, किन्तु जीव दशा में तृतीय नेत्र निमीलित हो जाता है। इसकी स्थिति भाल, अर्थात् भ्रूमध्य में मानी जाती है।शाक्त दर्शन
>>>पंचसूतक>धर्मशास्त्रों में जनन, मरण, रज, उच्छिष्ठ तथा जाति से पाँच प्रकार के सूतक माने गये हैं, अर्थात् घर में किसी का जन्म या मृत्यु होने पर, घर की किसी स्त्री के रजस्वला होने पर सूतक की प्राप्ति होती है। अतः इस सूतक के समय उस घर में पूजा आदि वैदिक कर्मो का निषेध किया गया है।वीरशैव धर्म में भी एक पात्र से अनेक लोगों के द्वारा पादोदक स्वीकार करने पर भी उच्छिष्ठ-सूतक नहीं होता। गुरु या जंगम के भोजन से अवशिष्ट अन्न को प्रसाद कहते हैं। इस प्रसाद के स्वीकार करने में भी उच्छिष्ठ सूतक नहीं हैउन्होंने शिवदीक्षा-संपन्न व्यक्ति किसी भी जाति का हो, उनके साथ समता का व्यवहार करने को कहा है।वीरशैव दर्शन
>>>पति>स्वामी। शिव। पाशुपत दर्शन में इस जगत के सृष्टिकर्ता व स्थितिकर्ता को पति कहा गया है। जो पशुओं अर्थात् समस्त जीवों (अर्थात् उनके सूक्ष्म तथा स्थूल शरीरों) की सृष्टि करता है तथा उनकी रक्षा करता है, वह पति कहलाता है। पति विभु है, वह अपरिमित ज्ञानशक्ति व क्रियाशक्ति से संपन्न है। अपनी इस अपरिमित तथा व्यापक शक्ति से पति इस जगत का सृष्टि व स्थिति कारण बनता है। पति की ही शक्ति से समस्त पशुओं (जीवों) का इष्ट, अनिष्ट, शरीर, स्थान आदि निर्धारित होते हैं। अर्थात् पति ही समस्त विश्व का एकमात्र संचालक है। पशु अथवा जीव के समस्त कार्यों पर स्वामित्व ही पति (ईश्वर) का पतित्व होता है। पाशुपत शैव दर्शन
>>>पुत्रकदीक्षा>यह दीक्षा साधक को सद्यः आगे ले चलने वाली उत्कृष्ट प्रकार की क्रिया-दीक्षा होती है। इसमें बाह्य आचार के नियम ढीले पड़ जाते हैं और आंतरयोग का अभ्यास स्थिर होने लग जाता है। इस दीक्षा का पात्र बना हुआ शिष्य पुत्रक कहलाता है। ऐसा शिष्य उस गुरु के पुत्र तुल्य माना जाता है। यह दीक्षा सभी पाशों से छुटकारा दिलाने वाली है तथा एकमात्र प्रारब्ध कर्म को छोड़कर शेष सभी भूत और भविष्यत् कर्मों का भी शोधन कर देती है। काश्मीर शैव दर्शन
>>>पंचम पुरुषार्थ है भक्ति> जीवन की सार्थकता के लिए मानव द्वारा अर्थ्यमान (प्रार्थित) होने से पुरुषार्थ कहा जाता है। यद्यपि अन्यत्र धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष नामक चार ही पुरुषार्थ माने गए हैं, किंतु वल्लभ दर्शन के अनुसार भक्ति भी एक स्वतंत्र पंचम पुरुषार्थ है और यह पुरुषार्थों में सर्वोत्कृष्ट है। वल्लभ वेदांत दर्शन
>>>प्रकृति> सत्व-रजः-तमः की समष्टि प्रकृति है। 'प्रकृति से सत्त्वादि उत्पन्न या आविर्भूत हुए', ऐसे शास्त्रीय वाक्य गौणार्थक होते हैं। 'प्रकृति' का अर्थ है - उपादानकारण। सांख्यीय दृष्टि से मूल प्रकृति के विकार असंख्य हैं (यथा महत्तत्त्व संख्या में असंख्य हैं), पर मूल प्रकृति एक है। कोई भी विकार प्रकृति से पृथक् नही है। सत्त्वादिगुण भी परस्पर मिलित ही रहते हैं। प्रकृति की दो अवस्थाएँ हैं - साम्यावस्था एवं वैषम्यावस्था। वैषम्यावस्था कार्य-अवस्था है, यह 'व्यक्त' नाम से अभिहित होती है। व्यक्त प्रकृति महत् आदि तत्त्वों के क्रम में है।सांख्य-योग दर्शन
>>>प्रत्याहार>अष्टांग योग में प्रत्याहार का स्थान पंचम है; कई योगग्रन्थों में प्रत्याहार को 'विषयों से इन्द्रियों को प्रयत्नपूर्वक हटा लेना' कहा गया है। इस 'हटा लेना' मात्र को पतंजलि ने प्रत्याहार नहीं कहा। उनके अनुसार 'शब्दादि विषयों से चित्त जब प्रतिनिवृत्त होता है जब इन्द्रियों के भी निवृत्त होने पर उनकी चित्त-स्वरूप के अनुकरण-सदृश जो अवस्था होती हैं वह प्रत्याहार है (2/54)। सांख्य-योग दर्शन
>>>बुद्धि> सांख्ययोग में बुद्धि शब्द दो अर्थों में प्रचलित है - (1) ज्ञान अर्थात् वृत्तिरूप ज्ञान तथा (2) बुद्धितत्व अर्थात् महत्तत्त्व । यह ज्ञान इन्द्रिय का धर्म नहीं है, किन्तु बुद्धि का धर्म है। सांख्ययोग में कुछ ऐसे स्थल हैं, जहाँ महत्तत्त्व या चित्त आदि शब्दों का प्रयोग न कर बहुधा बुद्धि शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। महत्तत्त्वरूप बुद्धि प्रकृति का प्रथम विकार है। सांख्य-योग दर्शन
>>>बुद्धि तत्त्व> सत्त्वगुण प्रधान महत्-तत्त्व। मूल प्रकृति में स्थित गुणों में विषमता के आ जाने पर सर्वप्रथम प्रकट होने वाला प्रमुख अंतःकरण। करण, ज्ञान तथा क्रिया के साधन को कहते हैं। व्यवहार में समस्त आंतर और बाह्य विषयों का निश्चयात्मक अध्यवसाय कराने वाला पुरुष का मुख्य अंतःकरण बुद्धि तत्त्व कहलाता है।काश्मीर शैव दर्शन
>>>बुद्धि प्रमाता>बुद्धि को ही अपना स्वरूप समझने वाला प्राणी। स्वप्न अवस्था में शरीर और बाह्य इंद्रियाँ सभी निष्क्रिय पड़े रहते हैं। फिर भी सारे उपादान, परित्याग आदि व्यापार तीव्रतर गति से चलते रहते हैं। उनको चलाने वाला तथा उनके चलाने के अभिमान को करने वाला सूक्ष्म शरीर रूपी प्राणी ही बुद्धिप्रमाता कहलाता है। यह प्रमाता अन्य सभी करणों के सूक्ष्म रूपों का उपयोग तो करता रहता है और प्राणवृत्तियों का भी उपयोग करता रहता है। फिर भी बुद्धिकृत संकल्प विकल्प आदि की ही इसमें प्रधानता रहती है, अतः इसे बुद्धि-प्रमाता कहते हैं। देहांतरों को यही प्रमाता धारण करता है और स्वर्ग नरक आदि लोकों की गति इसी की हुआ करती है। देवगण सभी बुद्धि प्रमाता ही होते हैं।काश्मीर शैव दर्शन
>>>बुद्धिवृत्ति>बुद्धि का व्यापार रूप परिणाम बुद्धिवृत्ति कहलाता है; विषय के संपर्क से ही बुद्धि से वृत्तियों का आविर्भाव होता है। बुद्धि चूंकि द्रव्य है, इसलिए वृत्ति भी द्रव्य है। वृत्ति को बुद्धि का धर्म कहा जाता है। यह वृत्ति वस्तुतः विषयाकार परिणाम ही है। बुद्धि चूँकि सत्वप्रधान है, अतः वृत्ति ज्ञान रूपा ही होती है; 'वृत्ति प्रकाशबहुल धर्मरूप है' ऐसा प्रायः कहा जाता है। यह ज्ञातव्य है कि बुद्धि से वृत्तियों के उद्भव में विषय आदि कई पदार्थों की आवश्यकता होती है, पर वह वृत्ति विषय आदि का धर्म न होकर बुद्धि का ही धर्म मानी जाती है, क्योंकि वृत्ति सत्त्वबहुल होती है। सांख्य में जो बुद्धिवृत्ति है, योग में उसको चित्तवृत्ति कहा जाता है ।सांख्य-योग दर्शन
>>>ब्रह्म> प्रपंच का बृंहण अर्थात् विस्तार करने के कारण तथा स्वयं बृहत् होने के कारण ब्रह्म कहा जाता है। यह ब्रह्म शब्द का योगार्थ है। वस्तुतः प्रपंच की उत्पत्ति, स्थिति और लय का कारण ब्रह्म है। ब्रह्म का यही लक्षण `जन्माद्यस्य यतः` इस सूत्र में प्रतिपादित किया गया है। उक्त सूत्र में प्रतिपादित यह लक्षण ब्रह्म का तटस्थ लक्षण है। सत्चित्त और आनंद (सच्चिदानन्द) यह ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है। नामरूपात्मक प्रपंच के अंतर्गत जैसे रूप प्रपंच के कर्त्ता ब्रह्म हैं वैसे वेद या नाम प्रपंच के भी विस्तार कर्त्ता ब्रह्म ही हैं। ब्रह्म का कार्य होने से वेद और नाम प्रपंच भी ब्रह्म शब्द से कहा जाता है ।वल्लभ वेदांत दर्शन
>>>ब्रह्म दृष्टि>`यह सब कुछ आत्मा ही है, यह सब कुछ ब्रह्म ही है`। 'सियाराम मय सब जग जनि' यह दृष्टि ब्रह्म दृष्टि है। उक्त दृष्टि प्रतीकात्मक (आरोपात्मक) नहीं है, किन्तु श्रवण के अनन्तर होने वाला मनन रूप है क्योंकि सभी वस्तु वास्तव में ब्रह्म ही है ।वल्लभ वेदांत दर्शन
>>> ब्रह्मचर्य> पंचविध यमों में यह एक है (योगसू. 2/30)। मनुष्य की त्रयोदश इन्द्रियों (पञ्च कर्मेन्द्रिय, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय तथा मन, बुद्धि व अहंकार) का संयम विशेषकर जिह्वा तथा उपस्था जननेन्द्रिय का संयम ब्रह्मचर्य कहलाता है। यह मुख्यतः उपस्थसंयम (मैथुनत्याग) है, यद्यपि अन्यान्य इन्द्रियों का संयम भी ब्रह्मचर्य में अन्तर्भूत है। उपस्थसंयम से शरीरवीर्य की अचंचलता अभिप्रेत है। वीर्यधारण से प्राणवृत्ति में सात्त्विक बल बढ़ता है, जो योगाभ्यास के लिए अपरिहार्य है। पाशुपतसूत्र के कौडिन्यभाष्य में जिह्वा और उपस्थ के संयम का विशिष्ट निर्देश दिया गया है। क्योंकि शेष ग्यारह इन्द्रियाँ इन्हीं दो से संबंधित होती हैं। जिह्वा व उपस्थ को मानव का शत्रु माना गया है, क्योंकि इन्हीं दो की प्रवृत्तियों से समस्त देहधारियों का पतन होता है। इन्द्रियों की प्रवृत्ति से, अर्थात् उनके किसी भी कर्म में प्रवृत्त होने से, दुःख उत्पन्न होता है, तथा उनके संयम में रहने से सुख होता है, क्योंकि जब इन्द्रियाँ प्रवृत्त नहीं होंगी तो किसी भी परिणाम की जनक नहीं बनेंगी। परिणाम, सुख अथवा दुःखपूर्ण, नहीं होगा तो सुख, दुःख दोनों आपेक्षिक भावों का जन्म नहीं होगा। अतः इन्द्रियों को संयम में रखना अतीव आवश्यक है। पाशुपत योग में ब्रह्मचर्य को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। ब्रह्मचर्य वृत्ति में धैर्य है, तप है। ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा होने पर योगी शिष्य के हृदय में ज्ञान का आधान करने में समर्थ होता है। व्याख्याकारों ने कहा है कि ब्रह्मचर्य का भंग आठ प्रकारों से होता है, स्मरण या श्रवण, कीर्तन, केलि, प्रेक्षण, गुह्यभाषण, संकल्प, अध्यवसाय तथा क्रियानिष्पत्ति। पुरुष के लिए स्त्रीसम्बन्धी बातों को सुनना या स्मरण करना तथा स्त्री के लिए पुरुष सम्बन्धी बातों को सुनना या स्मरण करना (रागपूर्वक, जिससे ब्रह्मचर्य की हानि होती है) श्रवण है। कीर्तन आदि को भी इसी प्रकार जानना चाहिए।सांख्य-योग दर्शन
>>>भक्ति> अनुभव-भक्ति साधक अहंकार शून्य होकर निरंतर ठाकुर - ध्यान में तत्पर होने के कारण 'भ्रमर-कीट-न्याय' से, अर्थात् जैसे कीट निरंतर भ्रमर-चिंतन से भ्रमर बन जाता है, वैसे यह साधक भी अपने में शिव-स्वरूप का अनुभव करने लगता है। इस शिवानुभव को शिव की ही कृपा समझना 'अनुभव-भक्ति' कहलाती है। यह भक्ति 'प्राणलिंगि-स्थल' के साधक में रहती है ।वीरशैव दर्शन
>>>भगवच्छास्त्र>श्रीमद्भागवत-गीता एवं पंचरात्र ये तीन भगवच्छास्त्र हैं। क्योंकि ये तीनों ही स्वयं भगवान् द्वारा उक्त हैं तथा भगवत्तत्त्व के प्रतिपादक हैं ।वल्लभ वेदांत दर्शन
>>>भजनानंद दान> भक्त की भक्ति के वशीभूत हुए भगवान् भक्त की इच्छा के अनुसार उसे सायुज्य आदि मुक्ति को न देकर भजनानंद प्रदान करते हैं। क्योंकि भक्त को मुक्ति से भी अत्यधिक अभीष्ट भगवान् के भजन से उत्पन्न आनंद है। अतः उसे ही वह चाहता है और भगवान उसे प्रदान करते हैं। यही भगवान् का भक्त के लिए भजनानंद दान है ।वल्लभ वेदांत दर्शन
>>>भवोद्भव> ईश्वर का नामांतर। भव (इस समस्त दृश्य जगत) का उत्पत्ति कारक होने के कारण ईश्वर को भवोद्भव कहा गया है। यद्यपि इस बाह्य जगत की उत्पत्ति जड़ प्रकृति तत्व से होती है। फिर भी उस तत्व को सृष्टि का कारण माना नहीं जाता है, क्योंकि वह तत्व स्वयं सृष्टि करने में समर्थ नहीं। उससे विश्व की सृष्टि तभी होती है जब ईश्वर उसमें से इस सृष्टि को करवाता है। अतः ईश्वर ही सृष्टि का प्रधान कारण है। अतः उसे भवोद्भव कहते हैं। उसे कारणकारणं भी कहते हैं । पाशुपत शैव दर्शन
>>>भाव > सात प्रकार के आचारों के समान ही तन्त्रशास्त्र के ग्रन्थों में त्रिविध भावों का भी विशद वर्णन मिलता है। ये हैं- पशुभाव, वीरभाव और दिव्यभाव। जन्मकाल से सोलह वर्ष तक पशुभाव, इसके बाद पचास वर्ष तक वीरभाव और पचास वर्ष के पश्चात् मनुष्य दिव्यभाव में रहता है। भावत्रय से अन्ततः भावों की सिद्धि होती है। ऐक्यभाव से साधक कुलाचार में प्रतिष्ठित होता है और इस कुलाचार के द्वारा ही मानव देवमय बन पाता है। भाव एक मानव धर्म है। मन ही मन सर्वदा उसका अभ्यास किया जाता है।
पशुभाव कामाख्यातन्त्र में पशुभाव का वर्णन करते हुए लिखा गया है कि जो प्रतिदिन हविष्य का आहार करते हैं, ताम्बूल नहीं छूते, ऋतु स्नाता अपनी स्त्री के सिवा अन्य किसी भी स्त्री को कामभाव से नहीं देखते, परस्त्री के कामभाव को देखकर उसका साथ त्याग देते हैं। पंचतत्व को स्वीकार नहीं करते और न उसकी निन्दा ही करते हैं, जो शिवोक्त कथा को सत्य मानते हैं, पाप कार्य को निन्दनीय समझते हैं, वे ही पशुनाम से प्रसिद्ध हैं। मत्स्य-मांस का सेवन कभी नहीं करते, गन्धमाल्य, वस्त्र आदि धारण नहीं करते, सर्वदा देवालय में रहते हैं और आहार के लिये घर जाते हैं। पुत्र और कन्याओं को अतिस्नेह दृष्टि से देखते हैं, ऐश्वर्य को नहीं चाहते, जो है उससे सन्तुष्ट रहते हैं। धन होने पर सदा दरिद्रों की सहायता करते हैं। कभी कृपणता, द्रोह और अहंकार नहीं दिखाते और जो कभी क्रोध नहीं करते, वे सब जीव पशुभाव में स्थित माने जाते हैं। रुद्रयामल तंत्र में लिखा गया है कि जो प्रतिदिन दुर्गापूजा, विष्णुपूजा और शिवपूजा करता है, वही पशु उत्तम है। शक्ति के साथ शिव की पूजा करने वाला भी उत्तम है। केवल विष्णु की पूजा करने वाला मध्यम और भूत-प्रेत आदि की उपासना करने वाला अधम है।
वीरभाव पिच्छिलातन्त्र प्रभृति में वीरभाव का वर्णन करते हुए लिखा गया है कि इस भाव में शक्ति या मद्य, मत्स्य, मांस, मुद्रा और मैथुन के बिना पूजा नहीं की जाती। स्त्री का भग पूजा का आधार है। यहाँ स्वर्ण अथवा रजत का कुश बनाया जाता है। कलियुग में मुख्य द्रव्यों के अभाव में अनुकल्प का भी विधान है। अथवा मानस भावना से ही सारी विधियाँ पूरी की जा सकती हैं। स्नान, भोजन, स्वकीया अथवा परकीया स्त्री, मद्य, मांस, स्वयंभू कुसुम, भगपूजन प्रभृति सभी विधियाँ यहाँ मानसिक भावना द्वारा ही सम्पन्न की जाती हैं। कलिकाल में मनुष्य संशयों से ग्रस्त रहता है। वह वास्तविक वीरभाव का अधिकारी नहीं हो सकता। अतः मानस भावना से ही उसको अपने इष्टदेव की उपासना करनी चाहिये। निशंक वीर ही वीर या दिव्यभाव का अधिकारी होता है। पंचमकार साधन, श्मशानसाधन, चितासाधन जैसी क्रियाएँ दिव्य या वीरभाव स्थित साधक के द्वारा ही सम्पन्न की जा सकती हैं।
दिव्य और वीर ये दो महाभाव हैं, पशुभाव अधम है। वैष्णव को पशुभाव से पूजा करनी चाहिये। शक्ति मन्त्र में पशुभाव भीतिजनक है। दिव्य और वीर भाव में वस्तुतः अन्तर नहीं है, किन्तु वीरभाव अति उद्धत है। रुद्रयामल में बताया गया है कि पशुभाव स्थित साधक किसी एक सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। किन्तु कुलमार्ग अर्थात् वीरभाव स्थित योगी अवश्य ही सब प्रकार की सिद्धियों का अधिकारी हो जाता है। महाविद्याओं के प्रसन्न होने पर ही वीरभाव की प्राप्ति होती है और वीरभाव के प्रसार से ही दिव्यभाव प्रकट होता है। वीरभाव और दिव्यभाव को ग्रहण करने वाले साधक वाञ्छाकल्पतरुलता के स्वामी हो जाते हैं, अर्थात् जब जो चाहे सो प्राप्त कर सकते हैं।
यह जगत देवतामय है। समस्त जगत स्त्रीमय और पुरुष भगवान् शिव है। इस प्रकार अभेद भाव से जो चिन्ता करता है, वह देवतात्मक या दिव्य है। उसको चाहिए कि वह नित्य स्नान, नित्य दान, त्रिसन्ध्या जप-पूजा, निर्मल वसन परिधान, वेदशास्त्र, गुरु और देवता में दृढ़ आस्था, गुरु मन्त्र और पितृ-पूजा में अटल विश्वास, बलिदान, श्राद्ध और नित्य कार्य का नियमित आचरण, शत्रु-मित्र में समभाव रखते हुए अन्य किसी के भी अन्न का ग्रहण न करे। शरीर यात्रा के लिये केवल गुरु (ब्रह्म) निवेदित अन्न स्वीकार करे। कदर्थ और निष्ठुर आचरण का परित्याग कर दिव्यभाव से सदा परमेश्वर की उपासना में निरत रहे। उसको सदा सत्य बोलना चाहिये। जो कभी असत्य का सहारा न ले वह साधक दिव्यभाव में स्थित माना जाता है। सत्ययुग और त्रेता के प्रथमार्ध तक दिव्यभाव की स्थिति मानी जाती है।शाक्त दर्शन
सोहन लाल द्विवेदी की वह कविता जो सोशल मीडिया पर हरिवंश राय बच्चन के नाम से मशहूर हो गयी
लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती,
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
नन्हीं चींटी जब दाना लेकर चलती है,
चढ़ती दीवारों पर, सौ बार फिसलती है।
मन का विश्वास रगों में साहस भरता है,
चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है।
आख़िर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती,
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।।
डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है,
जा जा कर खाली हाथ लौटकर आता है।
मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में,
बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में।
मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती,
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।।
असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो,
क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो।
जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम।
संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम।।
कुछ किये बिना ही जय जय कार नहीं होती।
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।।
>>>भूतकंचुकी>पृथ्वी आदि से बने हुए इस स्थूल शरीर रूपी चोले (कंचुक) को धारण करने वाला ज्ञानी साधक जब तक प्रारब्ध कर्म के भोगों को पूरा नहीं कर पाता है तब तक वह इस संसार से छुटकारा न पाता हुआ यहीं जीवन्मुक्त की अवस्था में निवास करता रहता है। परंतु उसे यह निश्चय हुआ होता है कि वह शुद्ध और परिपूर्ण संवित्स्वरूप ही है तथा यह पंच भौतिक शरीर उसका एक चोला मात्र ही है, वास्तविक स्वरूप नहीं है। इस तरह से शरीर को कंचुकवत् मानने वाला जीवन्मुक्त योगी है। काश्मीर शैव दर्शन
>>>महत्तत्त्व> महत्तत्त्व प्रकृति का सांख्योक्त प्रथम विकार है। सभी विकारों का बीजभूत होने के कारण यह 'महत्' कहलाता है - ऐसा प्रतीत होता है। इसी का नामान्तर बुद्धितत्त्व है। यह व्यावहारिक आत्मभाव का सर्वसूक्ष्म रूप है - 'अहमस्मि' बोध से ही यह लक्षित होता है। यह अभिमान से विहीन है। सास्मित समाधि में ही यह तत्त्व साक्षात्कृत होता है। अध्यवसाय महत् का लक्षण है - ऐसा पूर्वाचार्यों ने कहा है। महत्तत्त्व के साक्षात्कारी योगी ऐश्वर्यसंस्कार से युक्त होकर ब्रह्माण्डसृष्टिकारी प्रजापति हो सकते हैं। महत्तत्त्व एवं आत्मा इन दोनों की समष्टि 'महदात्मा' कहलाती है।सांख्य-योग दर्शन
>>>माया> सर्वभवन सामर्थ्य रूपा भगवान् की शक्ति माया है। माया शब्द के सामान्यतः चार अर्थ होते हैं, सर्वभवन सामर्थ्य रूप शक्ति, व्यामोहिका शक्ति, ऐन्द्रजालिक विद्या तथा कापट्य या कपटभाव। इनमें प्रथम शक्ति भगवान् की माया है ।वल्लभ वेदांत दर्शन
>>>मायाशक्ति > परमेश्वर की परिपूर्ण एवं अनिरुद्ध स्वातंत्र्य शक्ति। इसे पराशक्ति या परा मायाशक्ति भी कहा जाता है। यह परमेश्वर की स्वभावभूत परमेश्वरता ही है। परमेश्वर की ज्ञान, क्रिया तथा माया नामक तीन सर्वप्रमुख शक्तियों में से तीसरी शक्ति। ये ही तीन शक्तियाँ पशु भूमिका में तीन गुणों के रूप में प्रकट हो जाती हैं। इस तरह से तमोगुण का मूल स्वभाव भूत पारमेश्वरी शक्ति को भी मायाशक्ति कहते हैं। पशुभाव में भी स्वभावभूत ऐश्वर्य को प्रकाशित करने वाली पराशक्ति ही जब शुद्ध स्वरूप को आच्छादित करने वाली बन जाती है तो उसे भी मायाशक्ति कहते हैं। इस शक्ति से प्रभावित जीव पूर्ण भेद दृष्टि वाला बन जाता है, अपने-आपको शुद्ध संविद्रूप न समझता हुआ शून्य, बुद्धि या शरीर रूपी जड़ पदार्थ को ही अपना आप समझने लग जाता है। यही शक्ति माया तत्त्व नामक प्रथम जड़ तत्त्व को अवभासित करने वाली मानी गई है। काश्मीर शैव दर्शन
>>>मुक्ति>अपने विषय में शिवभाव का दृढ़तापूर्वक अभिमनन ही मुक्ति है। निश्चयपूर्वक और विश्वासपूर्वक यह ज्ञात हो जाना कि मैं वस्तुतः शुद्ध, असीम एवं परिपूर्ण परमेश्वर ही हूँ। संपूर्ण विश्व को अपनी ही शक्तियों का विलास समझना। मुक्ति अशरीर देखिए विदेह मुक्ति। मुक्ति जीवन देखिए जीवनमुक्ति। मुक्ति विदेह अशरीर मुक्ति। अपने शिवभाव का दृढ़तापूर्वक पूर्ण निश्चय हो जाने के अनंतर देह त्याग देने पर प्राप्त होने वाली सर्वथा अभेदमयी मुक्ति। इस अवस्था में विदेह मुक्त परिपूर्ण परमेश्वरता को प्राप्त कर लेता है। उसकी पृथक् सत्ता कोई रहती ही नहीं, प्राक्तन् पृथक् सत्ता ही सर्वथा असीम बनकर शिवसत्ता के रूप में चमकने लग जाती है।काश्मीर शैव दर्शन
>>>मुक्ति-आभास>प्रलयाकल या विज्ञानाकल की अवस्था को प्राप्त कर लेने पर जो प्राणी उसी अवस्था को वास्तविक मुक्ति समझने लगते हैं उन्हें वास्तविक मुक्ति तो प्राप्त होती नहीं है परंतु वे यही समझते हैं कि वे मुक्त हो गए हैं। उनकी इस स्थिति को मुक्ति आभास कहते हैं। मायाशक्ति के प्रभाव से ये उसी दशा को मुक्ति समझकर उसी के प्रति अनुरक्त हो जाते हैं जो दशा वस्तुतः मुक्ति की दशा नहीं होती है।काश्मीर शैव दर्शन
>>>मूलप्रकृति> मूलभूत प्रकृति मूलप्रकृति है। मूलभूत कहने का अभिप्राय यह है कि कुछ ऐसी भी प्रकृतियाँ हैं, जो इस प्रकृति के कार्यरूप हैं तथा यह प्रकृति अन्य किसी पदार्थ की विकाररूप नहीं हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि सत्त्व आदि तीन गुणों की जो साम्य-अवस्था है, वही मूल प्रकृति है, क्योंकि अन्य सब प्रकृतियाँ (महत्त्त्व, अहंकारतत्त्व तथा पाँच तन्मात्र) इस प्रकृति का ही साक्षात् या परम्पराक्रम से विकारभूत हैं।सांख्य-योग दर्शन
>>>मोक्ष>मोक्ष का शब्दार्थ है मोचन अर्थात् सर्वप्रकार के दुःखों से चिरकाल के लिए मुक्ति। इसी दृष्टि से मोक्ष को 'दुःखों की अत्यन्त निवृत्ति' कहा जाता है। दुःख चूंकि सहेतुक है, अतः हेतु के न रहने पर दुःख का उदय (अभिव्यक्ति) नहीं होगा। मोक्ष में दुःख के हेतु का अभाव होने से दुःखाभाव होता है पर यह मोक्षरूप अवस्था अभाव रूप नहीं है। दुःखाभाव एक अवस्थाविशेष का फल है, जिस अवस्था का वर्णन भावरूप से पूर्वाचार्यों ने किया है। यह अवस्था वस्तुतः 'द्रष्टा पुरुष का स्वरूपावस्थान' है (स्वरूप-प्रतिष्ठा या चितिशक्तिः - योगसूत्र 4/34)। इस अवस्था में बुद्धिगत वैषम्य-प्राप्त त्रिगुण साम्यावस्थ हो जाते हैं - इस दृष्टि से भी मोक्षावस्था अभावरूप नहीं है। स्वरूपतः भावरूप होने पर भी अभावरूप से इस अवस्था का प्रतिपादन किया जा सकता है, क्योंकि मोक्ष में पुरुष का वृत्तिसारूप्य नहीं रहता।सांख्य-योग दर्शन
>>>मोहकारिणी>जो शक्ति अपने आश्रय को विपरीत ज्ञान के द्वारा मोहित करती है, उसी को मोहकारिणी कहा जाता है। इसको अधोमाया या अविद्या भी कहते हैं। यह अविद्या शक्ति आणव आदि मलत्रय से जीव को आवृत करती है, जिससे कि वह अपने व्यापक स्वरूप को भूलकर अणुता का अनुभव करता है और अनित्य, अशुचि तथा दुःखमय शरीर आदि को नित्य, शुचि और सुखमय मानकर मोह में पड़ जाता है। अतएव इसे मोहकारिणी कहा जाता है। इस अविद्या के कारण ही जीव अनेक प्रकार के कर्म करता हुआ उन कर्मफलों को भोगने के लिये अनेक प्रकार की योनियों में भ्रमण करता रहता है। वीरशैव दर्शन
>>>लोपामुद्रा विद्या> लोपामुद्रा सन्तान और कामराज सन्तान के नाम से त्रिपुरा सम्प्रदाय के दो मुख्य विभाग हैं। लोपामुद्रा सन्तान की प्रवृत्ति अगस्त्य मुनि की पत्नी लोपामुद्रा से मानी जाती है। लोपामुद्रा ने ही सर्वप्रथम इस विद्या को लोक में प्रवृत्ति किया था। इसलिये उन्हीं के नाम से यह विद्या प्रसिद्ध हुई। हादिविद्या का अभिप्राय भगवती त्रिपुरसुन्दरी के उस मन्त्र से है, जिसका आरंभ हकार से होता है। दिव्यौघ, सिद्धौघ और मानवौघ क्रम से यह विद्या आज भी लोक में प्रवृत्त है। प्रपंचसार और सौन्दर्यलहरी में पहले हादिविद्या का ही उद्धार किया गया है।
>>>वरणभेद>एक जाति की वस्तु को जब योगी संकल्पबल से अन्य जाति में रूपान्तरित करते हैं तब जिस प्रक्रिया के आधार पर वह वस्तु अन्य जाति में परिणत होती है उस प्रक्रिया का परिचय 'वरणभेद' शब्द से योगसूत्रकार ने दिया है (4/3)। वरणभेद का अर्थ है वरण (= प्रतिबन्ध) का नाश। सूत्रकार का कहना है कि किसी वस्तु में जिस जाति की अभिव्यक्ति करानी है उस जाति की प्रकृति वस्तु में पहले से ही रहती है, पर विरुद्ध प्रकृति उसकी अभिव्यक्ति को रोके रहती है। इस आवरण (वरण) को भंग कर देने मात्र से सूक्ष्म रूप से अवस्थित अभीष्ट प्रकृति स्वतः अभिव्यक्त हो जाती है - इस अभिव्यक्ति के लिए अन्य कोई व्यापार पृथक् रूप से नहीं करना पड़ता। उदाहरणार्थ, धर्माचरण से तामस आवरण नष्ट होता है और सत्त्वप्रधान प्रकृतियाँ व्यक्त होती हैं। उसी प्रकार अधर्म से सात्त्विक आवरण नष्ट होता है और तमःप्रधान प्रकृतियाँ व्यक्त होती हैं। ये धर्म-अधर्म प्रकृतियों को प्रवर्तित नहीं करते, केवल उनके आवरणों का नाश करते हैं - यह वरणभेद है।सांख्य-योग दर्शन
>>>विवेक >'विवेक' शब्द का अर्थ है - पार्थक्य, भेद। लक्षणा से 'विवेक' का अर्थ पार्थक्यज्ञान भी होता है। योगशास्त्र में इसका अर्थ है - बुद्धि तत्त्व एवं पुरुष के भेद का ज्ञान। योगग्रन्थों में इसके लिए 'सत्त्व-पुरुषान्यताख्याति' शब्द प्रायेण प्रयुक्त होता है। यहाँ यह ज्ञातव्य है कि सत्त्व-पुरुष का यह पार्थक्यज्ञान समाधिपूर्वक ही होता है; लौकिक मनन से यह भेद यथार्थतः निश्चित नहीं हो सकता। शास्त्र के आधार पर भी सामान्य विवेकज्ञान ही होता है। पुरुष (अपरिणामी तत्त्व) प्रकृति (त्रिगुण) से पृथक् है - यह ज्ञान भी विवेक कहलाता है।सांख्य-योग दर्शन
>>>विभूति पाद> योग साधनों के श्रद्धापूर्वक किये गए अनुष्ठान से प्राप्त होने वाली विविध प्रकार की सिद्धियों अर्थात विभूतियों का वर्णन इस तृतीय पाद में मुख्य रूप से किया गया है इसी कारण इस पाद का नाम विभूति पाद है।
>>>विवेकजज्ञान>विवेकजज्ञान एक सिद्धि (विभूति) है, जिसका स्वरूप योगसूत्र 3/52 -54 में दिखाया गया है। ज्ञेयवस्तु के सभी धर्मों का ज्ञान इससे होता है। यह क्रमहीन है - अर्थात् युगपत् सभी धर्मों का ज्ञान इससे होता है। क्षण और उसके क्रम में संयम करने पर यह ज्ञान प्रकट होता है। चूंकि वस्तुगत क्षणिक परिणामों का ज्ञान इस सिद्धि में होता है, अतः योगी सर्वज्ञ हो जाते हैं (क्षणिक परिणाम ही सूक्ष्मतम परिणाम है)। यही कारण है कि सदृश वस्तुओं में जो भेद हैं, उसका परिज्ञान सिद्ध योगी को होता है। जातिभेद से, लक्षणभेद से तथा देशभेद से पदार्थों में भेदज्ञान होता है। जिन वस्तुओं में ये तीन भेद नहीं होते, उनमें भेदज्ञान नहीं हो सकता (साधारण व्यक्तियों में)। ऐसी वस्तुओं में भी विवेकजज्ञानवान् योगी को भेदज्ञान होता है (योगसूत्र 3/53)। विवेकजज्ञान विवेक अर्थात् प्रकृति-पुरुष के भेद के ज्ञान से भिन्न है। सांख्य-योग दर्शन
क्षणतत्क्रमयोः संयमाद्विवेकजं ज्ञानम् ॥ ३.५२॥
अन्वय -क्षण-तत्-क्रमयो:, संयमात् , विवेकजं, ज्ञानम् ॥
शब्दार्थ > क्षण- समय की सबसे छोटी इकाई को क्षण कहते हैं-मेरा अपना अनुभव कहता है -'moment of truth' (निर्णायक क्षण, सत्य का क्षण या मौत का क्षण ?), तत्क्रमयो: - क्षण एवं क्षण की निरंतरता में, संयमात् - संयम करने से, विवेकजं – विवेकज (विवेक से उत्पन्न), ज्ञानम् - ज्ञान (मृत्यु नश्वर शरीर और अहं की है, 'मेरी' अर्थात अविनाशी आत्मा की नहीं) की प्राप्ति होती है।
[क्षण क्रमाश्रित होने से कोई वस्तु नहीं है। एक क्षण के पीछे दूसरे क्षण का आना क्रम कहलाता है। योगीजन इसीको काल कहते हैं। दो क्षण एक साथ नहीं हो सकते और क्रम से भी दो क्षण एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि पूर्व वाले क्षण से उत्तर वाले क्षण का अन्त न होना ही क्षणों का क्रम है। इसलिए वर्तमान ही एक क्षण है, पूर्व और उत्तर क्षण नहीं हैं। इसलिए इन दोनों का एकत्व भी नहीं है। अतीत और अनागत क्षण वर्तमान क्षण का ही परिणाम कहने योग्य है। उस एक वर्तमान क्षण से ही सम्पूर्ण लोक परिणाम होते हैं। वास्तव में एक वर्तमान क्षण ही सत्य है। सब धर्म उस एक क्षण के ही आश्रित हैं। उसी एक क्षण का परिणाम सम्पूर्ण ब्रहमाण्ड बताया गया है। ऐसा जो एक वर्तमान क्षण है और उसका जो यह कल्पित क्रम हैं, उसमें संयम करने से विवेकज -ज्ञान उत्पन्न होता है। इसलिए क्षण और उसके क्रम में संयम करने से इन दोनों का साक्षात्कार पर्यन्त विवेकज-ज्ञान उत्पन्न होता है ।
(साभार @ https://shastragyan.in/https://
@#archive.org/stream/in.ernet.dli.2015.479874/2015.479874.Purano-me_djvu.txt]
व्याख्या > क्षण एवं क्षण कि निरंतरता (sequence) में संयम करने से योगी को विवेकज ज्ञान की प्राप्ति होती है ।
By making samyama on moment and it's sequence, one gains discriminative knowledge.
जातिलक्षणदेशैरन्यतानवच्छेदात् तुल्ययोस्ततः प्रतिपत्तिः ॥ ३.५३॥
>>>वीरेश> जाग्रत, स्वप्न तथा सुषुप्ति नामक तीनों अवस्थाओं का भोग करने वाला तथा तुर्या अवस्था में प्रविष्ट हुआ साधक। सृष्टि त्रिगुणात्मक है। प्रकाश, प्रवृत्ति तथा मोह क्रमशः सत्त्व, रज तथा तम में प्रधानतया चमकते हैं। शैव दर्शन के अनुसार जाग्रत्, स्वप्न तथा सुषुप्ति में क्रमशः तम, रज तथा सत्त्व प्रधानतया अभिव्यक्त होते है। इस प्रकार तीनों गुणों की साम्यावस्था रूप तुर्या में प्रवेश पाकर जब साधक शेष तीनों अवस्थाओं में स्वच्छंद रूप से विचरण कर सकता है तब उसे वीरेश कहते हैं। परमानंद से परिपूर्ण तथा भेदभाव को शांत करने में प्रवीण वीर इंद्रियों का स्वामी।
>>>वीरेश्वर>तीन गुणों से उद्भूत इंद्रिया समूहों द्वारा कल्पित विश्व का स्वेच्छापूर्वक सृष्टि और संहार में से विशेषतया संहार करने में व्यस्त वीरेश ही वीरेश्वर कहलाता है। काश्मीर शैव दर्शन
>>>वीर्य>ब्रहमचर्य की प्रतिष्ठा से होने वाला बल 'वीर्य' कहलाता है (द्र. योगसूत्र 2/38)। उपस्थसंयम के कारण शारीरसार की हानि न होने से, साथ ही अन्यान्य इन्द्रियों को संयत करने से प्राणशक्ति का सात्विक विकास होता है तथा मन में सात्विक प्रकाश विकसित होता है। यह विकास ही वीर्य है। इस वीर्य के कारण ही योगी में विभूतिविशेष का आविर्भाव होता है जिससे शिष्यों में ज्ञान का आधान करने में वह समर्थ होता है। 'नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः', इस कठोपनिषद्वाक्य में बल से यह वीर्य ही उक्त हुआ है।सांख्य-योग दर्शन
>>>शिवोടहं-भावना> मैं शिवस्वरूप हूँ' इस प्रकार की शुद्ध मानसिक चेष्टा को 'शिवोടहं भावना' कहा जाता है। शिव-ज्ञान के अनंतर इस भावना की आवश्यकता होती है, क्योंकि ज्ञान, ज्ञाता को ज्ञेय का परिचय कराता है; और भावना ज्ञाता को ज्ञेय स्वरूप बना देती हे। जैसे कीट को भृंग का ज्ञान होने मात्र से वह भृंग नहीं होता, किंतु अनवरत उसी का ध्यान करते रहने से वह भी भृंग बन जाता है।
उसी प्रकार शिवज्ञान होने मात्र से जीव शिवस्वरूप नहीं होता, किंतु शिवोടहं भावना से वह भी शिव बन जाता है। यहाँ पर भावना का अर्थ है निदिध्यासन। इससे ध्याता के विपरीत ज्ञान की संपूर्ण निवृत्ति हो जाती है, अर्थात् इस शिवोടहं-भावना से 'मैं अणु हूँ,' 'मैं अल्पज्ञ हूँ' इस प्रकार का उसका विपरीत ज्ञान निवृत्त हो जाता है और ध्याता जीव शिवस्वरूप बन जाता है। इसीलिये इस भावना को आंतरिक चक्षु कहा गया है।
>>>श्रीचक्र> महाशक्ति त्रिपुरा जब स्वेच्छा से अपनी स्फुरता को देखना चाहती है, तब श्रीचक्र के रूप में इस सृष्टि का उदय होता है। कामकला के प्रसंग में काम (रवि), बिन्दु और अग्नीषोमात्मक बिन्दुद्वय की चर्चा आई है। कामबिन्दु शून्याकार तथा बिन्दुद्वय विसर्गाकार है। इस बिन्दु और विसर्ग में लीलाभाव के जग जाने पर इन तीनों बिन्दुओं में स्फुरता की लहरी उठने लगती है, उनमें स्पन्दन होने लगता है और परस्पर एक दूसरे की ओर ये बहने लगती हैं। बहकर ये एकाकार हो जाती हैं, त्रिकोण का रूप धारण कर लेती है। इसी को बिन्दु और विसर्ग की लीला कहा जाता है।
>>>संवित्> शुद्ध चैतन्य। परप्रमातृ तत्त्व। समस्त भावजगत संवित् में ही संवित् के ही रूप में रहता है। जो कुछ भी जिस भी रूप में आभासित होता है वह सभी कुछ संवित् के ही कारण वैसा आभासित होता है क्योंकि संवित् जो कि शुद्ध एवं परिपूर्ण प्रकाश है उसके बिना और कुछ भी नहीं है और भासमान सारा प्रपंच उसी का बाह्य आकार है।
>>>संसार वृक्ष>संसार एक ऐसा आदिवृक्ष है, जिसकी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये आठ शाखायें हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चार रस हैं। दश इन्द्रियाँ जिसके पत्ते हैं, जिस पर जीव और ईश्वर रूप दो पक्षी हैं, सुख और दुःख रूप दो फल हैं तथा देहवर्ती नव द्वार ही जिसके कोटर हैं।